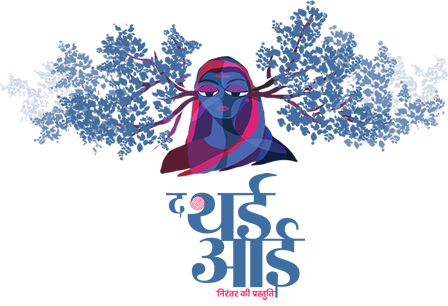“आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक बच्चे की तरह है. अगर हम उसे गलत जानकारी देंगे तो वो गलत ही सीखेगी.” ये ह्यूमंस इन द लूप फ़िल्म में उसकी मुख्य किरदार नेहमा अपनी सुपरवाइज़र से कहती है. उसने देखा कि ट्रेनिंग वीडियो में इल्ली के कीड़े को एक कीटाणु की श्रेणी में रखा गया है. नेहमा का मानना है कि ये गलत है. इल्ली सिर्फ सड़े हुए पत्तों को ही खाती है. असल में, वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती.
नेहमा, झारखंड में एक डेटा एनोटेशन सेंटर में काम करती है, जहां विदेशी कंपनियों के AI को बेहतर बनाने के लिए डेटा फीड करने का काम किया जाता है.
नैतिकता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर आज बहुत तरह की बहसें हो रही हैं. इन सबके बीच निर्देशक अरण्य सहाय की फ़िल्म ‘ह्यूमंस इन द लूप’ झारखंड के एक सुदूर इलाके में AI को निरंतर बेहतर बनाने के काम – डेटा लेबलिंग, में जुटी महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके अदृश्य श्रम को सामने लाने का काम करती है.
डेटा लेबलिंग, अपरिष्कृत डेटा, जैसे – चित्र, शब्द, वीडियो आदि की पहचान करने और संदर्भ प्रदान करने के लिए एक या अधिक सार्थक और सूचनात्मक लेबल जोड़ने की प्रक्रिया है ताकि मशीन लर्निंग मॉडल उससे सीख सके. झारखंड में ये महिलाएं विदेशी कंपनियों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए अलग-अलग तरह के लाखों चित्रों के नाम फीड करने का काम करती हैं.
2022 में फिफ्टी टू (Fifty two) नाम की एक वेबसाइट पर ‘ह्यूमन टच (इंसानी स्पर्श) नाम से एक निबंध प्रकाशित हुआ था. इस निबंध की लेखक करिश्मा मेहरोत्रा का कहना है कि सीखने-सिखाने की मशीन आधारित बनावट में ‘डेटा की समस्या’ सबसे प्रमुख है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्रान्ति ला दी है. आपके पास जितना अधिक डेटा हो – चित्र, वीडियो, शब्द – और वह जितना सटीकता से लेबल किया गया हो, एल्गोरिदम उतना ही अधिक परिष्कृत होने की संभावना रखता है.
एक सच यह भी है कि जाने-अनजाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए डेटा लेबलिंग का काम हम सभी ने भी किया है और कर भी रहे हैं. जब गूगल आपसे कैपचा (CAPTCHA) भरने को कहता है, या आप इंसान हैं या रोबोट इसमें फर्क करने के लिए बक्से में दिखाई दे रहे चित्र में ट्रैफिक लाइट की फोटो पर क्लिक करने के लिए कहता है, तो ये डेटा लेबलिंग है. कहीं न कहीं ऐसा करते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी निभा रहे होते हैं.
वर्तमान में भारत, AI के लिए डेटा फीड करने का सबसे बड़ा बाज़ार है. भारत में आईटी इंडस्ट्री एसोशिएसन नैशकॉम (NASSCOM) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाज़ार 126 अरब तक पहुंच जाएगा. 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में 70 हज़ार के करीब लोग काम कर रहे थे और ये लगभग 230 करोड़ डॉलर का बाज़ार था. इसमें 60 फीसदी से अधिक रिवेन्यू अमेरिका से तैयार हो रहा था. उस वक्त भारत से सिर्फ 10 फीसदी तक की ही डिमांड होती थी.
नैशकॉम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी साझा किया है कि इस फील्ड में काम करने वालों में लगभग 80 फीसदी कर्मचारी ग्रामीण, कस्बाई या पिछड़े इलाकों से आते हैं. जो कंपनियां इसमें काम करती हैं उनमें 90 फीसदी या तो टीयर 2 या टीयर 3 शहरों जैसे रांची, शिलॉन्ग, वाइजैक, भुवनेश्वर और येम्मिगनूर में स्थित हैं. किसी भी समय इन जगहों पर काम करने वाले लोगों में 50 फीसदी से अधिक महिला कर्मचारी होती हैं. भारत में डेटा लेबलिंग से जुड़ी कार्यप्रणालियों की जांच करने वाले एक अखबार के अनुसार, डेटा को फीड करने और उसकी पहचान करने के काम से जुड़े लोगों को इस काम में न के बराबर फायदा होता है. जबकि जिन कंपनियों के लिए ये लोग काम करते हैं, उन्हें बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है. उदाहरण के लिए, इस काम को करने वाले कर्मचारियों की औसत अवधि 12-18 महीने की होती है, जिससे स्थिरता और दीर्घकालिक करियर विकास के बहुत कम मौके मिलते हैं.
‘ह्यूमंस इन द लूप’ (2024) हिंदी-कुरुख भाषा में बनी फ़िल्म है जिसके निर्देशक अरण्य सहाय हैं. करिश्मा मेहरोत्रा के निबंध ‘ह्यूमन टच’ पर आधारित यह फिल्म म्यूज़ियम ऑफ इमैजिंड फ्यूचर (MOIF – एमओआईएफ) के साथ मिलकर बनाई गई है. यह तकनीक और समाज के मेल पर केंद्रित है. स्टोरीकल्चर इम्पैक्ट फेलोशिप के तहत विकसित एमओआईएफ एक ऐसा मंच है जहां रचनाकार, शोधकर्ता और कार्यकर्ता कहानी कहने के ज़रिए हमारे समाज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं.
फ़िल्म के बारे में:
‘ह्यूमंस इन द लूप’ फ़िल्म की कहानी नेहमा के इर्द-गिर्द घूमती है. वो एक आदिवासी महिला है, जो अपने दो बच्चों, 12 साल की लड़की धानू और 1 साल का लड़का गुन्टू, के साथ अपने मां-बाप के घर लौट आई है. नेहमा का तलाक हो चुका है. घर के पास ही वो डेटा लेबलिंग का काम करती है – एक ऐसा काम जहां वो तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए AI की मदद करती है, उन्हें सही तरीके से पहचानने में. नेहमा को लगता है कि AI भी बच्चों की तरह सीखता है और अपनी कल्पनाओं में वो दुनिया को AI की नज़र से देख रही होती है जो असल दुनिया में वो अपनी बेटी धानु के साथ महसूस करना चाहती है.
धानू शहर जाने की ज़िद करती रहती है इसलिए नेहमा के लिए उसे गांव में रोकना मुश्किल हो जाता है. जब नेहमा अपनी बेटी को गांव में रुकने की वजहें बताने की कोशिश करती है तब उसे महसूस होता है कि AI भी इंसानों की तरह पक्षपाती बनने लगा है और उसके समुदाय के खिलाफ जो भेदभाव है, वह AI में भी दिखने लगा है. आखिरकार नेहमा को समझ आता है कि तलाक के बाद न सिर्फ उसे धानू की कस्टडी या उसके भविष्य के लिए लड़ना है बल्कि इस बात के लिए भी लड़ना है कि तकनीक और समाज उसके जैसे लोगों को कैसे देखते हैं.
द थर्ड आई के साथ अपनी फ़िल्म पर बात करते हुए निर्देशक अरण्य सहाय ने फ़िल्म के बनने की कहानी, इसके पीछे किए गए शोध, लेखन और सबसे महत्त्वपूर्ण कि उन्होंने ये कहानी कहना क्यों चुना – इन विषयों पर विस्तार से बात की. यहां पेश है इस बातचीत से महत्त्वपूर्ण अंश:
टीटीई: आप फ़िल्म बनाने की दुनिया में कैसे आए?
अरण्य सहाय: मेरी दुनिया सोशल साइंस की दुनिया है. मैंने राजनीतिक विज्ञान से अपनी पढ़ाई पूरी की है. मेरी मां समाजशास्त्री हैं. मुझे शोध बहुत पसंद है. खासकर तब जब शोध मुझे अलग-अलग जगहों पर जाकर वहां का हो जाने में मदद करता है… तो मुझे लगता है कि फ़िल्में बनाना इसी नज़रिए से आया है – अपने माहौल से बाहर निकलकर भारत को समझने की कोशिश करना, जहां हैं, उसे समझना. हम जहां भी रहते हैं, वहां इतनी सारी परतें होती हैं.
मैं एफटीआईआई (FTII- भारतीय फ़िल्म एवं तकनीक संस्थान) में पढ़ने गया. वहां मैंने कुछ शॉर्ट फ़िल्में बनाईं और बाद में डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाईं. ह्यूमंस इन द लूप (चक्र में घूमता इंसान) मेरी पहली फीचर फ़िल्म है. एफटीआईआई में मैंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम है- सॉन्ग फॉर बाबासाहेब (बाबासाहेब के लिए एक गीत).
ये एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है जो महाराष्ट्र के शाहिरी गीतों पर आधारित है. शाहिरी, महाराष्ट्र में प्रतिरोध के गानों का सबसे पुराना रूप है. महाराष्ट्र की नज़र से इसे देखें तो यहां की राजनीति इसे और खास बना देती है. यहां दो तरह की ताकतें या विचारधाराएं काम करती हैं – एक, जो सेंटर से राइट की तरह है और दूसरी, जाति विरोधी राजनीति की दमदार ताकत.
मैं पुणे में था और उस इलाके की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा था. तभी मैं दत्तवाड़ी पहुंचा. विदर्भ के इलाके में पानी की किल्लत की वजह से वहां के लोग इस इलाके में आकर बसने लगे. पूरी बस्ती एक नहर के साथ-साथ बसी है. तो मेरी जो चाहतें थीं कि एक जगह से उजड़कर नई जगह बसना, विस्थापन या माइग्रेशन, इसे अकादमिक लेखों या किताबों के ज़रिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के वास्तविक क्षणों में सामने से देख सकूं. ये सब ही था जिसने मुझे खोज की तरफ खींचा. मुझे लगता है कि वही मेरी किसी भी तरह की फ़िल्म बनाने की नींव बन गई.
‘ह्यूमंस इन द लूप’ फ़िल्म बनाने से पहले मुझे एक छोटा सा ग्रांट मिला था. यही वजह थी कि मैं झारखंड जाकर वहां एक साल रहकर शोध और लेखन कर सका. वहीं मेरी मुलाकात बिजू टोप्पो से हुई. बिजू, झारखंड के ही रहने वाले हैं और यहां की जन-जातियों एवं प्रकृति से जुड़े विषयों पर फ़िल्में बनाते हैं. उनकी फ़िल्मों के लिए उन्हेें तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है. बिजू का अपना एक फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है ‘अखरा’ और जो झारखंड में संस्कृति और संचार के क्षेत्र में काम करता है.
बिजू ने मुझे लेखकों, फ़िल्ममेकर्स और कला संरक्षणवादियों से मिलाया. इनसे मिलकर मैंने झारखंड की खास पहचानें, सोच-विचार, दर्शन, पूर्वजों के किस्से, ऐतिहासिक समझ के बारे में बारीकी से जाना. ये फैक्ट आधारित शोध से एकदम अलग चीज़ें हैं. इनके ज़रिए मैं झारखंड को नज़दीक से समझ पाया, उनके अनुभवों और नज़रियों को महसूस कर सका… और जिसे मैंने अपनी कहानी में भी शामिल किया. मुझे लगभग एक साल लगा शोध को फ़िल्म की स्क्रिप्ट के रूप में तैयार करने में.
टीटीई: आपने अपनी फ़िल्म में डेटा लेबलिंग के ज़रिए कहानी कहने की कोशिश की है. ये डेटा लेबलिंग क्या है, और इससे फ़िल्म को कैसे देखा जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा बताएं.
अरण्य सहाय: यह कहानी कहने की सबसे बढ़िया शुरुआत है, पर अक्सर यही कहानी के लिए एक अभिशाप बन जाता है. आपके हाथ जैसे बंध जाते हैं क्योंकि फिर लोग इसी आधार पर फ़िल्म के बारे में बात करते हैं, कहानी पर ध्यान ही नहीं देते, “वाह, हमको नहीं पता था कि ऐसा भी होता है!” मैं नहीं चाहता कि कोई फ़िल्म सिर्फ इसी आधार पर देखी जाए.
उदाहरण के लिए कॉन्टेंट मॉडरेशन नाम की एक चीज़ होती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, और ऑनलाइन गेम्स में, उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सामग्री की समीक्षा करने और उसे प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है. उसके बारे में ये तय किया जाता है कि सामुदायिक मानकों के आधार पर ये ‘देखने लायक’ वीडियो है या नहीं. मैं अपनी कहानी को उधर लेकर जाना चाहता था, फिर मुझे लगा कि इससे मैं खुद को सीमित कर दूंगा क्योंकि हिंसा आसान तरीका है ध्यान खींचने और बनाए रखने का. तो, फिर मैंने सोचा कि मैं इससे ज़यादा कुछ कर सकता हूं, तभी मैंने डेटा लेबलिंग को समझना शुरू किया.
अगर एक इंसान हज़ारों फोटो और वीडियो को देखकर बार-बार उसे टैग करता है, और उसी के आधार पर कोई एल्गोरिदम यह सीखता है कि कुर्सी और मेज़ में क्या फर्क है तो क्या यह मां-बाप की तरह पालन-पोषण करने जैसा ही है? जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि किसी रंग या वस्तु में कैसे फर्क कर सकते हैं और साथ ही अपनी नैतिकता और दुनिया को देखने का तरीका भी सिखाते हैं. AI के संदर्भ में मुझे यही पैटर्न देखने को मिला.
यहां एक आदिवासी मां है जो एक AI बच्चे को सिखाने का काम कर रही है, फर्क इतना है कि वो विकसित देश (फर्स्ट वर्ल्ड) के डेटा और लेबल के आधार पर उसे सिखा रही है. ये लेबल अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से संदर्भित होते हैं, है ना?
एक के लिए जो कीट है, वह दूसरे के लिए कीट नहीं है. ‘कीट’ शब्द एक मूल्य आधारित शब्द है. फ़िल्म में जो महिला डेटा लेबल कर रही है उसने देखा है कि वो कीट फसलों की रक्षा करता है, तो वो ये कैसे मान ले कि वह नुकसान पहुंचाता है? यही सवाल है.
क्या AI सच में वैसा क्लीन स्लेट है जैसा लोग इसके बारे में सोचते हैं या ये हमारे पूर्वाग्रहों, हमारी कमज़ोरियों और ज्ञान की व्यवस्थाओं की ही संतान है? एक तरफ ये सोचने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि AI अजीवित लोगों की एक दीर्घकालिक सभ्यता हो सकता है जो आगे जाकर दूसरे ग्रहों और अंतत: पूरे ब्रह्मांड पर छा जाएगा. पर असल में इसका जन्म ही उस डेटा से हुआ है जो हमने उसमें डाला है; हम उसके अकेले संरक्षक है जिनके ज्ञान पर वो बड़ा हो रहा है.
पहले मैं AI को ऐसा कुछ मानता था जिसे संभाल कर रखने की ज़रूरत है – और अब भी मानता हूं. मैं उन तकनीक विचारकों जैसी सोच ही रखता था जो मानते हैं कि पृथ्वी पर जैविक जीवन बहुत नाज़ुक है. एक बड़ा हादसा, जैसे किसी उल्का का टकराना या परमाणु युद्ध, इंसानियत और जैव विविधता, सबको मिटा सकता है. उस संदर्भ में,

अगर AI ऐसी तबाही से बच सकता है, तो वह पृथ्वी का वारिस बन सकता है. पर अगर AI को पृथ्वी का वारिस बनना है, तो क्या उसे सिर्फ एक ही नज़रिए या जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करना चाहिए?
वॉएजर 1, जो अभी भी अंतरिक्ष में उड़ रहा है, उसमें जो गोल्डन डिस्क है उसमें 3 या 4 रागों से ज़्यादा नहीं हैं लेकिन उसमें अमेरिका के अलग-अलग इलाकों के बहुत सारे गाने हैं. हम जानते हैं कि राग भी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते. हमारे यहां तो लोक संगीत में भी बहुत गहराई में जाकर ही समझ में आता है कि किस तरह का संगीत है. ए.के. रामानुजन ने इसपर बहुत सुंदरता से बात की है – ‘छोटी परंपराएं’ और ‘बड़ी परंपराएं’ और उनका आपसी संबंध. छोटी परंपराएं भी उतनी ही अहम हैं. और जैसा कि उन्होंने बताया, बहुत से राग खेतों में गाए गए गीतों से जन्मे हैं: औरतें खेतों में गा रही हैं, वहीं से एक राग जन्म लेता है. क्या हमने इसका अध्ययन किया है? क्या हमें पता भी है कि यह संगीत के विकास का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं.
साथ ही, अब मेरा नज़रिया बहुत बदल गया है. अभी हम एजीआई (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) के निर्माण की वैश्विक दौड़ के बीच हैं जो पश्चिम और चीन के बीच चल रही है और यह दौड़ सोच-समझकर होने वाले विकास के मुकाबले नंबर 1 होने पर केन्द्रित है. यह एक गंभीर संभावना को जन्म देता है कि हम ऐसा एजीआई बना सकते हैं जो हमें बचाने के बजाय हमें ही मिटा दे.
लेकिन इन सारी बातों को आप एक भावनात्मक कहानी के साथ ही कह सकते हैं नहीं तो फिर ये बौद्धिक या अकादमिक चर्चाओं में ही रह जाएगा.
टीटीई: आपने फ़िल्म में ये कैसे सुनिश्चित किया कि आदिवासी पारिस्थितिक ज्ञान जिसे आप फ़िल्म में लेकर आ रहे हैं, वह किरदार की मानसिकता का हिस्सा बने? फ़िल्म के अंत में आप ज्ञान के बारे में असल में क्या कहना चाहते हैं?
अरण्य सहाय: ये बहुत सारी आदिवासी महिलाओं के साथ बातचीत से निकल कर आया. मैं एक उरांव आदिवासी कलाकर फिलोमिना तिर्की इमाम से बात कर रहा था. फिलोमिना, बुलु इमाम की पत्नी हैं, जो एक आदिवासी संरक्षणविद हैं जिन्होंने 70 गुम हुई नवपाषाणकालीन शैल कला की जगहों की खोज की है. फिलोमिना ने बताया कि जब आप घास पर चलते हैं तो आपको लगता है कि ये आपका हक है. पर, हम घास का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें अपने ऊपर चलने दिया. तो, जब हम उनके नज़रिए से देखते हैं तो उसमें एक बहुत गहरा विश्वास दिखाई देता है. हम एक बहुत गहरे विश्वास के साथ ही जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, जो हमारी मानसिकता का हिस्सा होता है. ये गहरे विश्वास जब नए अनुभवों में बदलते हैं, तो वही फ़िल्म का विषय है. एक आदिवासी व्यक्ति (ज़रूरी नहीं कि सभी आदिवासी) यह मानता है कि एक बड़ा दार्शनिक विचार है कि हर चीज़ में जीवन होता है.
व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हमारे आसपास हर एक चीज़ में चेतना होती है. अगर आप उसका आदर नहीं करते तो ब्रह्मांड आपको इसकी सज़ा देता है. जब नेहमा, जो कि एक आदिवासी लड़की है, जिसके पिता ने उसे सिखाया है कि हर एक चीज़ में ज़िंदगी है, वो जब AI के आकार को देखती है, तो उसे स्वाभाविक रूप से लगता है कि इसमें भी ज़िंदगी है. जो आदिवासी नहीं है वो शायद ऐसा सोचे भी नहीं.
तो जब उसे लगता है कि वो ज़िंदा है और वो एक बच्चा है, तो आपको उसे सिखाना होगा. आपको उसे सही तरीके से बड़ा करना होगा. वरना हम AI से बिना भावना के जुड़ सकते हैं क्योंकि वह ऑटोमेशन है, वह सिर्फ डेटा है, वह निष्प्राण है. वह शरीर से इतना दूर है और आप उसे देख भी नहीं सकते. यह कुछ ऐसा है जिसे आप समझने की कोशिश करते हैं, और फिर भी नहीं समझ पाते.
टीटीई: क्या आपको लगता है कि फ़िल्म AI के विमर्श में उसकी तरफ एक सकारात्मक रवैया रखती है?
अरण्य सहाय: एक तरह की सकारात्मकता तो ज़रूर है, पर इसके पीछे दो-तीन कारण हैं. पहला कारण है कि आपको डिजिटल लेबर और AI के पहलूओं को अलग-अलग देखना होगा. डेटा का जो काम है, जब आप इसे थोड़ा दूर से देखते हैं तो ये शोषणकारी दिखाई देता है. लेकिन जब आप इन औरतों से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके पास एक नौकरी तो है. इससे पहले उनके पास कोई काम नहीं था. कमरे के भीतर बैठकर, कुर्सी-मेज़ पर कम्प्यूटर पर काम करने में एक तरह के सम्मान की भावना है, जो कि खेती में दिहाड़ी पर शोषण वाले काम करने के मुकाबले कई गुना बेहतर है.
दूसरा, ये मेरी हमेशा नई संभावनाओं की ओर देखने की व्यक्तिगत-राजनीतिक इच्छाओं से भी निकलकर आता है. यह उम्मीद की तरफ एक प्रस्ताव है, उस सोच से दूर कि कुछ नहीं हो सकता. चीज़ें कभी सही दिशा में नहीं जाएंगी लेकिन क्या हम उम्मीद से इंकार कर सकते हैं? हम उम्मीद से कैसे इंकार कर सकते हैं?
और आखिर में, ये फ़िल्म पहचान और ज्ञान प्रणालियों के बारे में है. लेकिन AI और प्रशासन के बारे में, AI और युद्ध के बारे में, AI और पुलिसिंग के बारे में भी इसके ज़रिए बात की जा सकती है. ये वो चीज़ें हैं जो मैं इस फ़िल्म में करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया.
लेकिन मैं एकदम नया काम लिख रहा हूं, जो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग और तकनीक के ज़रिए उसके होने के बारे में है. ऐसी जगह, जहां इंसान की किस्मत का फैसला AI निष्पक्षता से करता है… वह कहानी किसी और फ़िल्म के लिए है.
और मुझे लगता है कि इंसान का इसमें रहना ज़रूरी है. हम उन्हें (AI को) जानकारी देते हैं और वे हमें देते हैं. हम, जो रचनात्मक लोग हैं, हमें इस सब का एक मतलब निकालने की ज़रूरत है.
टीटीई: फ़िल्म की स्क्रीनिंग से जुड़ा कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहें?
अरण्य सहाय: एक स्क्रीनिंग के बाद सवाल जवाब के सेशन में एक सवाल मेरे ज़ेहन में अब भी है. किसी ने पूछा, “क्या आपको लगता है कि आदिवासी ज़िंदगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में एक जैसे हैं? क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं?” मैंने कहा, “यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं.” फिर उन्होंने कहा, “लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन खनिजों से AI चल रहा है, वे उन्हीं इलाकों से निकाले जा रहे हैं?” ये सोचने वाली बात है.
क्या आपको उम्मीद है कि ये फ़िल्म शिक्षकों या सीखने-सिखाने या ज्ञान की दुनिया में काम करने वाले लोगों के बीच किसी तरह की चर्चा को उभारने का काम कर सकती है?
अरण्य सहाय: जैसा कि फ़िल्म में दिखाया गया है. मैं चाहता हूं कि इस फ़िल्म में अपना सच कहने और अपनी कहानी सुनाने का अधिकार केंद्र में हो. साथ ही इस फ़िल्म में और भी कई विचार साथ-साथ चलते हैं. इसमें जो सबसे प्रमुख है वो प्रकृति के नियम और तकनीक की दुनिया का साथ-साथ रहना, जहां हम आदिवासी नज़रिए को ज़्यादा सुन सकें ताकि आगे का रास्ता निकल सके.
कार्यशाला
‘ह्यूमंस इन द लूप’ फ़िल्म कृत्रिम बौद्धिकता की बहुत सारी परतें हमारे सामने खोलती है. अगर आप अपने क्लासरूम या किसी कार्यशाला में एआई पर समझ को खोलना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म के ज़रिए शुरुआत की जा सकती है.
फ़िल्म की पटकथा में एक आदिवासी महिला है जो डेटा लेबलिंग का काम करती है. उसकी एक किशोरी बेटी है (जो मां से नाराज़ रहती है) और एक नन्हा सा बेटा है (जो अभी चलना सीख रहा है); इनके बैकग्राउंड में है एक डेटा लेबलिंग सेंटर. ये सारा दृश्य झारखंड में स्थित एक काल्पनिक कहानी में दिखाई देता है. फ़िल्म सवाल करती है कि आखिर किसका ज्ञान, ज्ञान समझा जाता है, और किसका नहीं? हम किसे ज्ञान मानते हैं?
इस कार्यशाला के ज़रिए ऐसे कई सवालों पर चर्चा की जा सकती है:
- क्या आपको अपने बचपन की कोई कविता, कहानी या कुछ और याद है जिसे आप हमेशा अपने भीतर संजो कर रखते हैं? उससे जुड़ी कौन सी यादें हैं और क्यों?
- क्या अपनी पढ़ाई या सीखने की प्रक्रिया के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि आप जो सीख रहे हैं उसमें आपकी पहचान भी शामिल है? अगर हां, तो वो क्या है? आप खुद को विशेषाधिकार के पिरामिड में कहां खड़ा पाते हैं? अगर नहीं, तो क्यों?
- खुद का या अपने समुदाय का कोई अनुभव जहां आपने जाना कि वह ज्ञान का स्रोत है पर उसकी पहचान इस रूप में नहीं होती है. इस बात पर थोड़ा सोचें और इसे सभी के साथ साझा करें.
- एक विद्यार्थी के रूप में जहां आप किताबों के ज़रिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे में एआई के ज़रिए चीज़ों के बारे में जानना कैसा महसूस होता है? ऐसा करते हुए किस तरह की इच्छाएं मन में आती हैं?
- एक ऐसे समय में जहां जानकारियों की अधिकता जितनी ज़्यादा है उतनी ही गलत जानकारियों का भरमार है, ऐसे में क्या सही है क्या गलत – इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं? आपकी नज़र में सच क्या है और झूठ क्या है?
- अगर आपको मौका मिले कि आप एक शिक्षक के रूप में आज की दुनिया के बारे में एक चैप्टर लिखें, तो वो क्या होगा?
कार्यशाला:
1. ‘ह्यूमंस इन द लूप’ से एक हिस्सा:
उपस्थित समूह में सभी लोग चैटजीपीटी/एआई (ChatGPT/AI) सॉफ्टवेयर की मदद से एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें. यह तस्वीर खुद के बारे में या अपने समुदाय के बारे में हो सकती है. इसके ज़रिए यह जानने की कोशिश करें कि एआई आपके या समुदाय के बारे में किस तरह की तस्वीर प्रस्तुत करता है. इसके लिए आप एआई के साथ इस संबंध में कुछ जानकारियां साझा कर सकते हैं. (अपनी भौगोलिक जानकारी, जाति/समुदाय, जेंडर आदि)
- आपको क्या पता चला?
- एआई से प्राप्त तस्वीर को देखकर आपने कैसा महसूस किया?
- एआई वाली तस्वीर और सच्चाई में कितनी समानता है?
- उपस्थित समूह में एआई को दी गई जानकारी के बारे में आपस में चर्चा करें: आपने क्या शब्द लिखे थे? आपने किस तरह की जानकारी को अधिक महत्त्व दिया और किसे कम महत्त्व दिया. और क्यों?
- क्या आप एआई द्वारा तैयार की गई तस्वीरों में कोई पैटर्न देख पा रहे हैं? एआई द्वारा निर्मित तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है और क्या छुपा हुआ है?
इस कार्यशाला का एक उद्देश्य यह है कि इसके ज़रिए हम डिजिटल में प्रतिनिधित्व की पहचान कर सकते हैं. साथ ही कृत्रिम तकनीक की इस नई दौड़ में हम देख सकें कि वास्तविक दुनिया की हमारी गैर-बराबरियां, भेदभाव, हमारे दुराग्रह किस तरह दिन-प्रतिदिन अपना रूप बदलते अभासीय दुनिया में भी हु-ब-हु देखने को मिल जाते हैं.
2. इसका एक प्रमुख उद्देश्य वस्तुओं के ज़रिए कहानियां कहना भी है.
- हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उसे नाम और पहचान देकर उसे अलग-अलग किया जाता है और जमा किया जाता है. क्या हो अगर हम डेटा को आभासीय न मानकर किसी वस्तु के रूप में देखें? इस एक्टिविटी के ज़रिए डेटा को एक वस्तु मानकार उसमें भावनाओं को जोड़कर देखने का प्रयास है. ऐसा करके हम किसी आम चीज़ पर ध्यान दे पाते हैं क्या? इस तरह उसके प्रति हमारी समझ और हमारी भावनाओं में कोई बदलाव आता है क्या?
- कमरे के चारों ओर देखिए और अपने आस-पास की जगह से 3 से 5 वस्तुओं को चुनिए. कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी वस्तु चुनें जो हाथ से बनी हो या जिसमें कुछ जीवंतता हो. हर वस्तु के लिए एक लेबल या एनोटेशन बनाइए. उदाहरण के लिए – आकार, साइज़, रंग, बनावट, उपयोग, उससे जुड़ी कोई याद या भावना वगैरह.
- उस वस्तु को एक जीवित प्राणी की तरह सोचिए: वह किस चीज़ की चाह रखती है? वह क्या याद करती है?
- अगर वह बोल सकती, तो क्या कहती? हर वस्तु के लिए एक छोटी कहानी लिखिए, जैसे कि उसकी जीवनी हो. इस तरह सोचिए कि आपको उस वस्तु को दुनिया से परिचित कराना है. आप इसमें कल्पना भी जोड़ सकते हैं.
अगर आप ये कार्यशाला करने में हमारी मदद चाहते हैं या आपने ये कार्यशाला की है, दोनों ही स्थितियों में आप हमें इस आईडी – [email protected] पर मेल कर इसके बारे में बता सकते हैं.
-
शिवम रस्तोगी द थर्ड आई में वीडियो प्रोड्यूसर और इमेज एडिटर हैं. वे एक फॉटोग्राफर और फिल्ममेकर हैं. वे लगातार कैमरा के पीछे से दुनिया और इसके विभिन्न रंगों को समझने की कोशिश करते रहते हैं. उन्होने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से जर्नलिज़्म और मास कम्यूनिकेशन में स्नातक की डिग्री और जामिया मिलिया के मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर से स्नाकोत्तर डिग्री हासिल की है. शिवम ने फिल्म कम्पेनियन और मेमेसयस कल्चर लैब के साथ काम किया है.
-
सामिया लेखक एवं शोधकर्ता है. किस्से-कहानियों के प्रति लगाव ने उन्हें अंग्रेज़ी साहित्य में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से अंग्रेज़ी में बी.ए की पढ़ाई पूरी कर, आंबेडकर विश्वविद्यालय से क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री हासिल की. शहरों को जानना, उसकी संस्कृति को समझना और कहानियां कहना सामिया को बहुत पसंद है. वर्तमान में वो द थर्ड आई के साथ सोशल मीडिया मैनेजर और संपादकीय सहायक के रूप में काम कर रही है. बारहमासा हॉट चॉकलेट की वकालत करने के अलावा, उन्हें अपनी अलमारी में खोई हुई पेंसिल या कलर को ढूंढ लेना पसंद है. कविताएं उनकी हमसफर हैं.