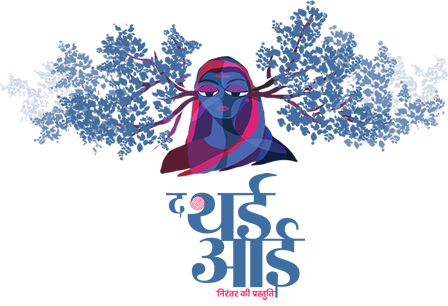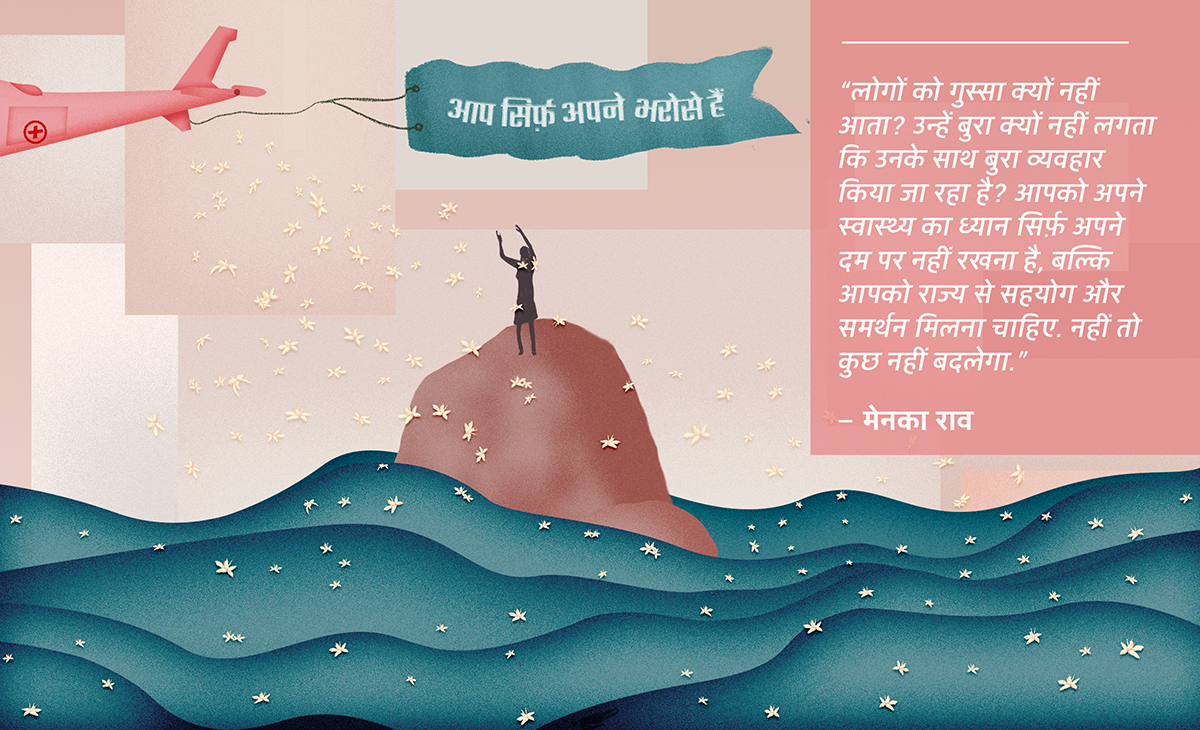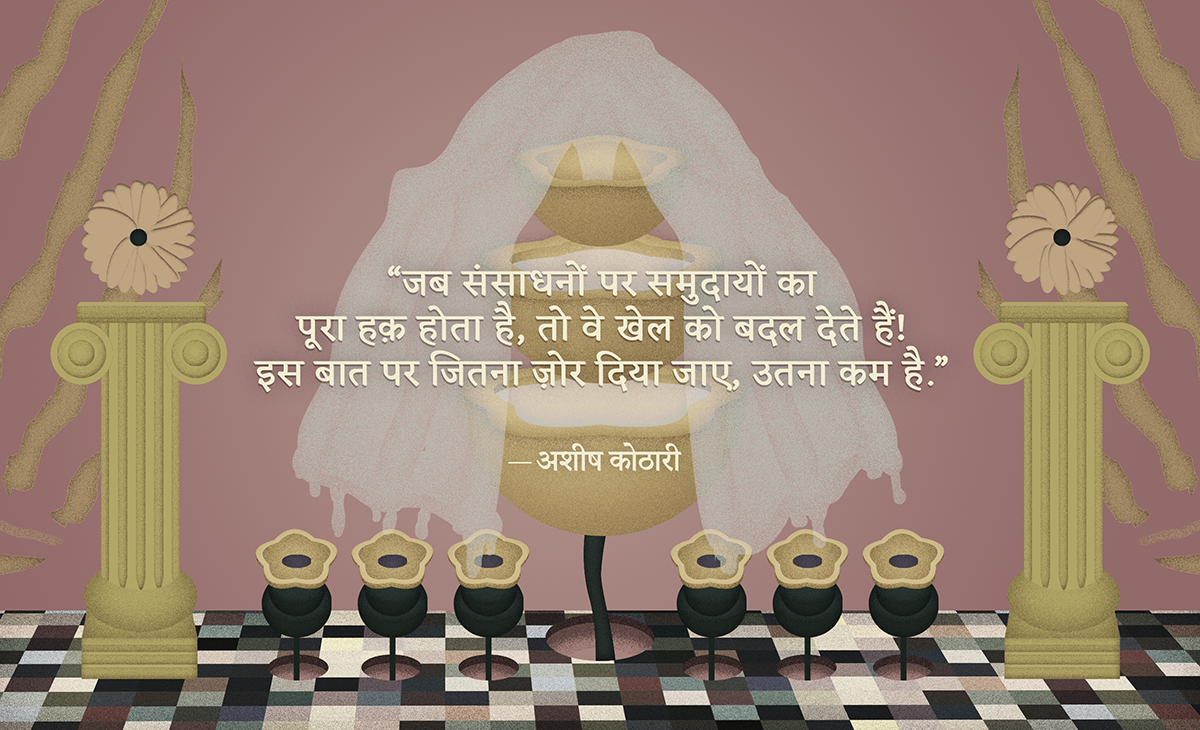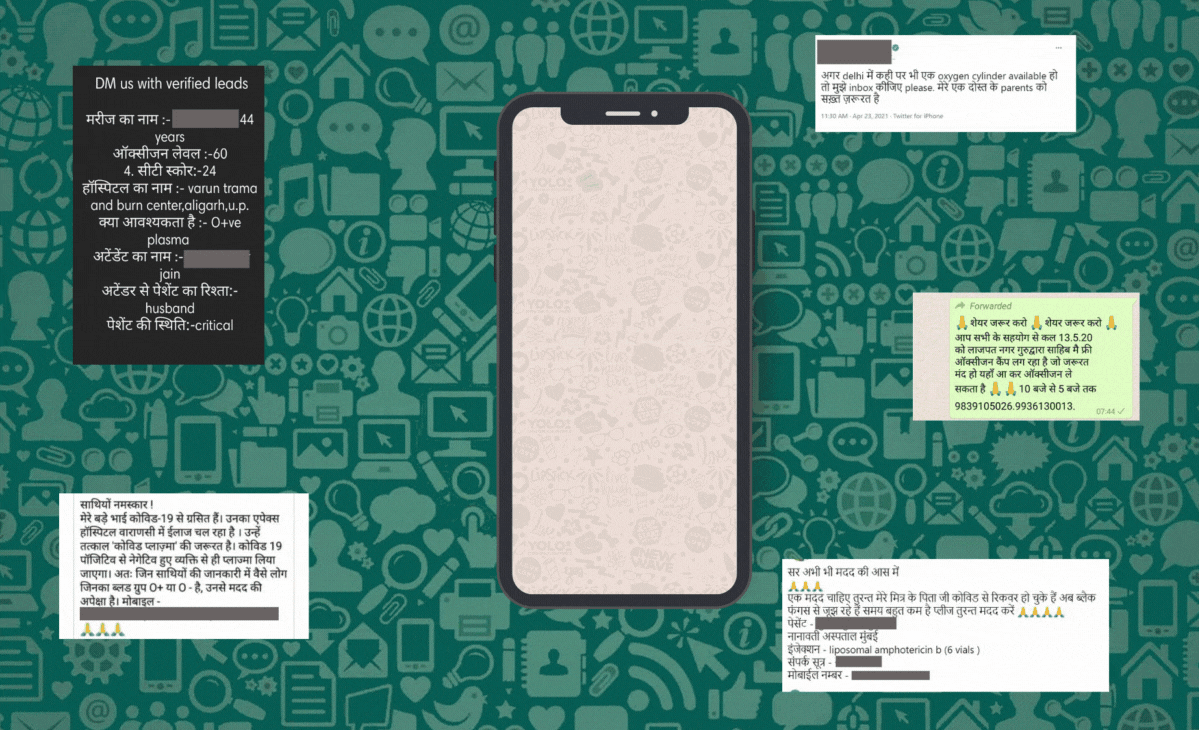“किसी व्यक्ति को भोजन के लिए दिन में तीन बार लाइन में खड़ा करना उन्हें अपमानित करना है.”
कर्नाटक के कार्यकर्ता, क्लिफ्टन डी’रोज़ारियो, ने यह साफ़ किया कि खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था टिक ही नहीं सकती. वे मंथन लॉ, बंगलुरू से जुड़े एक अधिवक्ता हैं और अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद (AICCTU) के राष्ट्रीय सचिव और सीपीआई (ML) लिबरेशन, कर्नाटक के राज्य सचिव हैं.