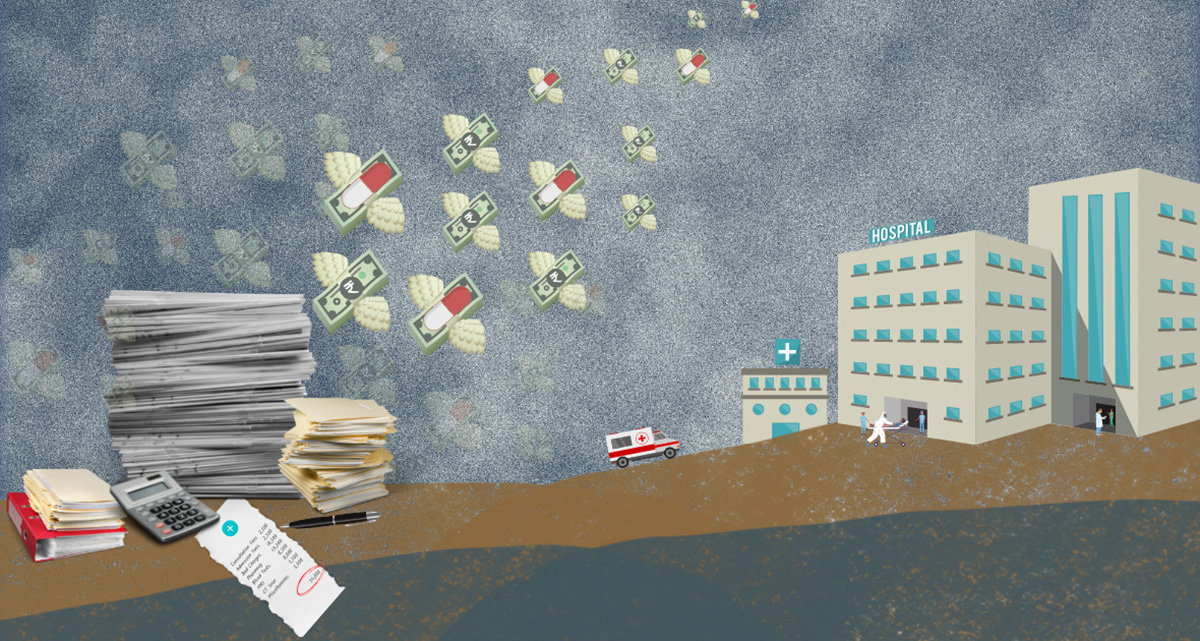रवि दुग्गल एक समाजशास्त्री, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं शोधकर्ता हैं. वे पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं. एक बार उन्हें बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. उस वक़्त वे जिस कंपनी के साथ जुड़े थे उसकी तरफ़ से कराई गई स्वास्थ्य बीमा योजना में वे 15 साल से प्रीमियम भर रहे थे और उसी के बूते वे मुम्बई के मशहूर जसलोक अस्पताल में भर्ती हुए. ऑपरेशन हुआ और कुल – 60,000 रुपए का बिल आया. लेकिन उनकी बीमा कंपनी ने सिर्फ़ 45,000 रूपए दिए.
बचे हुए 15,000 की रकम अपनी जेब से जमा करवाने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली. रवि बताते हैं, “मेरे पास सरकारी बीमा पॉलिसी है और मुझे अपने बाकी बचे पैसे लेने के लिए 6 महीने तक मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर बीमा वालों ने 15 में से 10 हज़ार की रकम मुझे और वापस की. अभी भी 5 हज़ार मैंने अपनी जेब से दिए. ये मेरे जैसे व्यक्ति की हालत है जिसे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे काम करती है या बीमा कंपनियां कैसे काम करती हैं, इसके बारे में सबकुछ पता है. प्रीमियम देने के बावजूद ज़रूरत पड़ने पर मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ा.”
अब सोचिए, ऐसा अगर, इतने जानकार व्यक्ति के साथ हो सकता है तो आम आदमी बीमा के इस उलझे हुए जाल से कैसे निकल सकता है?
जन स्वास्थ्य व्यवस्था विशेष संस्करण में हमने रवि दुग्गल से बात कर जाना कि क्यों आजकल स्वास्थ्य बीमा को एक ज़रूरत की तरह पेश किया जा रहा है? क्या हम स्वास्थ्य बीमा लेने और न लेने की दुविधा के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? रवि के साथ इस बातचीत के ज़रिए पढ़िए स्वास्थ्य बीमा के टेढ़े-मेढ़े और उलझे रास्ते से निकलने का सही रास्ता क्या हो सकता है.
रवि दुग्गल से यह साक्षात्कार जुलाई 2021 में किया गया था. यहां हम बातचीत से संपादित अंश साझा कर रहे हैं.
साक्षात्कारकर्ता : सोहनी हर्षे
भारत में प्राइवेट बीमा योजनाओं ने कब और कैसे कदम रखा?
वैसे तो भारत में निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का पर्दार्पण 1986 में होता है, लेकिन उस वक़्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही इसमें शामिल थीं जो जनता को अतिरिक्त सुविधाएं देने के नाम पर स्वास्थ्य सुविधाओं के ज़रिए उनकी मदद कर रही थीं. ये कंपनियां मुनाफ़ा नहीं कमा रही थीं.
इस तरह की मेडी-क्लेम पॉलिसी जो 1986-87 में चालू हुई उसका प्रीमियम भी बहुत कम होता था. क्योंकि मेडी क्लेम के पीछे मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक मदद और उन्हें अस्पताल, वहां भर्ती होने, इलाज़ कराने जैसी प्राइवेट सुविधाओं की आदत की लत लगाना ही लक्ष्य था.
गौर करने वाली बात है कि ये ख़ासतौर से मिडिल क्लास के लिए डिज़ाइन किया गया था. इसमें ग़रीब तबके के लोग शामिल नहीं थे.
कंपनियां, कर्मचारियों को मासिक स्वास्थ्य भत्ता देने से लेकर एचआर पॉलिसी के तहत मेडिकल खर्चे की एक तयशुदा रक़म वापस देने जैसी स्कीम लेकर आईं. लेकिन, कुछ ही समय में उन्हें समझ आ गया कि इतने कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं अगर बीमा के रूप में दी जाएं तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है. लोग ज़्यादा और ख़र्चा कम, इससे कंपनी का पैसा भी बचेगा! उन्होंने बीमा कंपनियों से सामूहिक बीमा के नाम पर प्रीमियम में मोलभाव कर उसे कम रखने की मांग की.
आज की तारीख़ में समूचे बीमा सेक्टर का 40 फीसदी हिस्सा सामूहिक बीमा से आता है, अगर इसमें उन सार्वजनिक बीमा योजनाओं को हटा दें जिनके लिए सरकार पैसा देती है. तो. कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की तरफ़ धकेला. आकर्षण यह कि कर्मचारी अपना इलाज जसलोक, हिन्दुजा या अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों में आसानी से करवा सकते हैं.
इस तरह बीमा पॉलिसी के ज़रिए आर्थिक मदद की चमक वाले लड्डू के आकर्षण में मिडिल क्लास ने सरकारी अस्पतालों से अपना पल्ला झाड़ लिया.
सार्वजनिक बीमा योजनाएं कब और कैसे आईं?
2008-09 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और कुछ राज्य आधारित बीमा योजनाओं का आगमन हुआ. इनके अंतर्गत सरकार ने कुछ विशेष राज्यों में ग़रीबी रेखा से नीचे गुज़र-बसर करने वाले लोगों के लिए थोक में बीमा योजनाओं की ख़रीद की. उस वक़्त सरकार ने प्रीमियम के पैसे को भी 500 से 600 रुपए तक रखने पर ज़ोर दिया, जो आज की तारीख़ में बहुत अधिक बढ़ चुका है. ये बहुत बड़ी बीमा योजना थी जिसे प्राइवेट सेक्टर की मदद से पूरा किया जा रहा था.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने स्वास्थ्य में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का रास्ता बनाया, क्योंकि एक तो ये सारा प्रीमियम का पैसा प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनियों के पास जा रहा था और दूसरा 80 फीसदी इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे थे.
फिर भी ये योजनाएं कम से कम ग़रीब जनता के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने का रास्ता तो हैं?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सिर्फ़ 30,000 रुपए के बीमा तक सीमित थी, जिसमें बड़ी बीमारियों से जुड़ा इलाज शामिल नहीं था. इसके अंतर्गत छोटा-मोटा इलाज, या कोई छोटा सा ऑपरेशन यही संभव हो सकता था.
इसके बाद कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, और आंध्र-प्रदेश – जो उस वक़्त बीमा आधारित कार्यक्रमों में लीडर की भूमिका निभा रहे थे – को देखते हुए 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) को लाया गया. लेकिन, एक दशक बीतते-बीतते इन राज्यों को समझ आ गया कि बीमा आधारित स्वास्थ्य योजनाएं एकदम फर्ज़ी हैं. ऐसे बहुत तरह के मामले सामने आए जिनमें पैसों के लिए बिना ज़रूरत लोगों की सर्ज़री कर दी गई.
विशेषज्ञों और दूसरे शोध के दस्तावेज़ों में ये बार-बार लिखा गया कि कैसे बीमा आधारित स्वास्थ्य योजनाओं से लोगों को उस तरह का फायदा नहीं मिला जैसा इसे लागू करते वक़्त सोचा गया था और आख़िरकार लोगों को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ रहा है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने का ही काम कर रही हैं.
लेकिन, अगर बीमा कंपनियां मेडिकल बिल का भुगतान कर रही हैं तो फिर लोगों की जेब से पैसा क्यों ख़र्च हो रहा है?
भारत में बीमा के बावजूद आपको अपनी जेब से पैसा ख़र्च करना ही पड़ता है. अगर, आप सरकारी अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेने जाएं तो आपको अपनी तरफ़ से पैसा ख़र्च करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर सरकारी अस्पताल में कह देते हैं कि – एक्स-रे मशीन ख़राब है बाहर से एक्स-रे करवा लें, ये दवाई हमारे यहां उपलब्ध नहीं बाहर से ले आएं, ये इंजेक्शन यहां नहीं मिलता और भी बहुत परेशानियां वे आपको गिना देंगे.
फ़िर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ़ मुड़ जाते हैं. प्राइवेट बीमा कंपनियां आपको बताती हैं कि आपकी स्कीम में ये सुविधाएं हैं, ये नहीं हैं. नतीजतन, बीमा होने के बावजूद लोगों को अपनी पॉकेट से भी अस्पताल का बिल भरना पड़ता है.
इसमें एक और सच्चाई है कि जैसे-जैसे लोगों के पास थोड़ा पैसा आने लगा है, वे प्राइवेट में इलाज करना ज़्यादा सही समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकारी अस्पतालों में या तो डॉक्टर नहीं मिलेगा या दवाइयां नहीं मिलेंगी. वे समझते हैं कि सरकारी जगह पर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि थोड़ा महंगा ही सही प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा लें, कम से कम वहां इलाज तो सही मिलेगा.
सरकारी संस्था एनएसएस की रिपोर्ट कहती है कि जिन राज्यों ने बीमा आधारित योजनाओं को लागू किया है वहां लोगों की जेब से ख़र्च बढ़ा है. ऐसा तमिलनाडु तक में हुआ है जहां सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं. रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि प्राइवेट सुविधाओं में तो स्वास्थ्य पर जेब से ख़र्च पांच गुणा तक बढ़ा है.
तमिलनाडु की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं देश में सबसे अच्छी है. उनके पास राज्य स्तर पर बीमा आधारित योजना थी उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना भी है जो पूरी तरह से बड़ी बीमारियों के इलाज पर ही आधारित है. तमिलनाडु ने अपनी स्वास्थ्य बीमा स्कीम को ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों तक के लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश की जिसे पूरा करने के लिए वे अपनी तरफ़ से पैसा लगा रहे हैं. लेकिन, 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में लोगों को अपनी जेब से भी स्वास्थ्य बिल का भुगतान करना पड़ रहा है. भले ही ये सारी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, लेकिन लोग या तो मजबूर हैं या वे सरकारी व्यवस्था की ख़राब हालत देखकर ख़ुद प्राइवेट सेक्टर की तरफ़ मुड़ जाते हैं.
आपके अनुसार फिर पब्लिक सेक्टर बीमा से किसे फ़ायदा मिलता है?
वे लोग जो अच्छा कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, घर है. ऐसे लोगों को ही इसका फ़ायदा मिल रहा है. इनकी संख्या जनसंख्या की कुल 15 फीसदी है जिनमें – सरकारी कर्मचारी, सांसद और हमारे नेता- मंत्रीगण शामिल हैं- इन सभी को सेंट्रल गर्वमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं मिलती हैं.
सेंट्रल गर्वमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में सरकार प्रति व्यक्ति 8,500 रुपए ख़र्च करती है. लेकिन यही सरकार, आम जनता के स्वास्थ्य के नाम पर प्रति व्यक्ति 1600 रुपए ख़र्च करती है. ज़ाहिर है कि CGHS स्कीम के ज़रिए सरकारी बेनिफेट पाने वाले लोगों को सभी तरह की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं – उन्हें अच्छे डॉक्टर्स, दवाइयां, केयर, सबकुछ मिल रहा है. यहां तक कि वे बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा सकते हैं.
कमाल की बात है कि सरकार ये भी नहीं बताना चाहती कि CGHS के अंतर्गत बजट जाता कहां है? मैंने आरटीआई के ज़रिए पता लगाना चाहा कि इसका पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसमें बाहर से प्राइवेट अस्पतालों की सुविधा लेने पर किसका फायदा होता है? लेकिन अबतक किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है.
वैसे, इस स्कीम में भी वरीयता के आधार पर भेदभाव है. डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के लिए बीमा की सुविधाएं ज़्यादा है वहीं क्लर्क के स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी के लिए उनके मुकाबले कम सुविधाएं उपलब्ध हैं. सेना में भी CGHS स्कीम है और जनरल से लेकर जवान तक वहां सभी के लिए एक बराबर सुविधाएं हैं. उनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है. यही चीज़ रेलवे के कर्मचारियों के साथ भी है. ये दोनों ही सरकारी बीमा सुविधा के मामले में बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं.
तो अब हमें पता है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 8000 रुपए प्रति व्यक्ति की दरकार है तो हम स्वास्थ्य मंत्रालय से यही उम्मीद करते हैं कि वे सभी के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने में इतना ही पैसा लगाएं.
स्वास्थ्य से जुड़ा सारा इतिहास यही कहता है कि हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुधारने एवं उन्हें ठोस बनाने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया. ख़ासकर शहरी इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो फ़िर भी कुछ थोड़ा बहुत केयर मिल जाता है, टीकाकरण हो जाता है, शहरी इलाकों में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं.
अगर, बीमा होने के बावजूद लोगों को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ रहा है जिसका नतीजा है कि भारी संख्या में लोग कर्ज़ और गरीबी की मार झेलने पर मजबूर हैं फिर बीमा लेने से क्या फ़ायदा?
बीमा पूरी तरह से फर्ज़ी चीज़ है. ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों के पास बीमा होने के बावजूद उन्हें कोविड का इलाज नहीं दिया गया. हमने जन स्वास्थ्य अभियान की तरफ़ से महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया कि वे प्राइवेट अस्पतालों का ऑडिट करवाए. सरकार ने हमारी बात मानकर ऑडिट करवाया जिसके बाद लगभग 15 करोड़ रुपए उन मरीज़ों को वापस दिए गए जिनसे अस्पताल ने मनमानी फ़ीस वसूली थी.
तो क्या ये लोगों की दिक्कत है कि उन्हें ठोस जानकारी नहीं होती कि स्वास्थ्य बीमा कैसे काम करता है या कैसे उसका फ़ायदा लिया जा सकता है? या फ़िर ये स्वास्थ्य बीमा के काम करने के तरीकों की बनावट में ही परेशानी है?
मेरे विचार से ये बीमा के ढांचे की कम और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर किसी तरह की सख़्ती के न होने की दिक़्कत ज़्यादा है जिसका फ़ायदा उठाकर वे मनमाने तरीके से काम करते हैं. जब डॉक्टर ही अनैतिक तरीके से काम करने लगेंगे और मनमाने टेस्ट लिखने लगेंगे तो इंश्योरेंस वाले इसे अपना हथियार बना लेते हैं. फ़िर वे हर चीज़ पर सवाल करने लगते हैं. एक तो हमारे यहां किसी भी इलाज का कोई एक मानक तरीका नहीं है. एक ही बीमारी का इलाज हर अस्पताल अपने तरीके से करता है. यही कारण है कि – बीमा लेने वाले व्यक्ति, बीमा कंपनी और अस्पताल- इन तीनों के बीच बहुत बड़ी खाई है.
मैं अपना उदाहरण दूं तो
ऑपरेशन के बाद जब मैं बीमा की रक़म लेने के लिए गया तो बीमा कंपनी ने मेरे मुंह पर मुझे कहा कि जसलोक अस्पताल तो दूसरे अस्पतालों के मुकाबले 30 फीसदी ज़्यादा पैसा चार्ज करता है. इसलिए बीमा की रकम देते वक़्त हमने उसमें से 30 फीसदी पैसा काट लिया था. अगर आप किसी और अस्पताल में इलाज करवाते तो हम ये पैसा नहीं काटते.
इसका तो यही मतलब हुआ कि उन्हें पहले एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि जसलोक अस्पताल या ब्रिच कैंडी अस्पताल नहीं जाएं, उसकी जगह इस-इस अस्पताल में अपना इलाज करवाएं तभी आपको बीमा के पैसे मिलेंगे.
अगर मान लें कि बीमा से जुड़ी सारी जानकारियां पहले से लोगों को मालूम हैं और प्राइवेट सेक्टर को इसका पालन भी करने को कहा जाए तो क्या ऐसे में बीमा सही है?
इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना को लेते हैं. इस योजना के तहत सभी तरह की जानकारियां पहले से मौजूद हैं – इतनी रक़म का बीमा है और उसमें इन-इन बीमारियों का इलाज शामिल हैं. अब मुझे और मेरे पूरे परिवार को मिलाकर मेरे पास एक साल में पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा है. बीमा की इस रक़म को हथियाने के लिए अस्पताल उन सारे हथकंडों का इस्तेमाल करने लगते हैं जिनसे बीमा की अधिकतम राशि उन्हें मिल जाए. भयानक तरीके से बिल बनाया जाता है. हमारा ऑडिट सिस्टम भी लोगों की तरह ही ग़रीब है. बीमा कंपनियों के पास ख़ुद का ऑडिट सिस्टम नहीं होता और जिन थर्ड-पार्टी सिस्टम के ज़रिए ऑडिट करवाया जाता वो प्राइवेट सेक्टर की ऑडिटिंग में पूरी तरह सक्षम नहीं होते. इससे होता यही है कि मरीज़ और अस्पताल दोनों के बीच अविश्वास बुरी तरह से फैल जाता है.
मेरा मानना है कि भारत में स्वास्थ्य बीमा का कोई भविष्य नहीं है, भारत ही क्यों विश्व के अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीमा से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ, ये कहीं काम नहीं करता.
अमरीका अकेला ऐसा देश है जिसके बारे में हमें पता है कि वहां बीमा बुरी तरह से फैला हुआ है और हमें ये भी पता है कि वो वहां की जनता की बर्बादी का एक बड़ा कारण भी है. फिलहाल वहां बीमा कंपनियों के पास ख़ुद के अस्पतालों की चेन है. अस्पताल से डॉक्टर बीमा कंपनी को फोन पर उनसे विचार-विमर्श करते हैं कि मरीज़ को क्या इलाज देना है. बीमा कंपनी के पास कोई डॉक्टरी अनुभव हो या न हो लेकिन वे बताती हैं कि नहीं ये वाला इलाज नहीं, वो इलाज दीजिए.
ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए?
प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना चाहिए, ये भी कि वे किस कीमत पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं. लेकिन, सरकार को इसके लिए पीपीपी (PPP) मॉडल या ऐसा कोई मॉडल नहीं लाना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाए. इसकी जगह पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो 6400 करोड़ रुपए का बजट है उसे ज़िला अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत करने में लगाना चाहिए. दरअसल, सरकार के पास सारी शक्तियां और साधन हैं किसी ज़िला अस्पताल को कॉलेज अस्पताल में बदलने के लिए लेकिन नीति आयोग का कहना है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के ज़रिए ही हो सकता है. इसका सीधा मतलब है – ज़िला अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना.
ऐसा नहीं होना चाहिए. सरकार को इसके लिए पैसा कहीं और से लाना चाहिए. सीएसआर के फंड का इस्तेमाल करें, माइनिंग मिनरल के विकास से जुड़े फंड का इस्तेमाल करें या जंगल फंड का इस्तेमाल करें – ये वे अकूत फंड हैं जिनका इस्तेमाल सरकार, कर्मचारियों की तनख़्वाह देने में कर रही है क्योंकि कोविड के बाद से टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई है.
जहां तक इंश्योरेंस की बात है
सरकार को चाहिए कि वह प्राइवेट सेक्टर के लिए बैसाखी का काम न करे, उन्हें अपने दम पर बाज़ार में काम करने दे. प्राइवेट सेक्टर को बाज़ार पर भरोसा है तो वे ख़ुद बाज़ार में अपना माल बेचें, सरकार की मदद न लें, लेकिन उन्हें पता है बिना सरकार की मदद के उनके बीमा प्रीमियम में काफी गिरावट आ जाएगी.
तो क्या लोगों को स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए?
मैं बहुत जगहों पर पब्लिक हेल्थ कोर्स पढ़ाता हूं. सभी जगह मैं स्टुडेंट्स को एक ही सलाह देता हूं कि – हेल्थ बीमा न लें. अभी वे जवान हैं. ये पैसा बीमा कंपनी को देने की बजाए वे इसे बैंक में आर.डी. (रेकरिंग डिपोज़िट) कर सकते हैं. आर.डी. में हर महीने उतना पैसा जमा करते जाएं जितना वे प्रीमियम में जमा करवाएंगे. आख़िर ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा तो आपका अपना होगा और उसपर ब्याज भी मिलेगा. नहीं तो ये इंश्योरेंस कंपनी हर साल आपका पैसा खाती रहेगी, और आपको कुछ नहीं मिलेगा.
ऐसे में “क्या होगा अगर” जैसी परिस्थितियां भी होती हैं जिसकी चिंता की वजह से लोग स्वास्थ्य बीमा लेने पर मजबूर हो जाते हैं. मान लीजिए इमरजेंसी हुई और मेरे बचत का सारा पैसा उसमें ख़र्च हो गया तो? ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य बीमा से कम से कम इलाज के एक बड़े हिस्से का पैसा चुकाया जा सकता है.
ऊपर जो मैंने सुझाव दिया वो दोतरफा रणनीति है. पहला, आप अपना पैसा जमा करते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे मेडिकल बिल को चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि 100 में से किसी 1 व्यक्ति के साथ कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाए और बचत खाते में पर्याप्त पैसा न हो. रिस्क हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग ज़रूरत के अनुसार पैसा जमा कर लेते हैं और उसी के अनुसार उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
दूसरी बात, मिडिल क्लास को भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहिए. ये कमोबेश मुफ़्त होती हैं. हम इस्तेमाल करेंगे तो व्यवस्था में सुधार भी आएगा.
हम चिल्लाएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अधिकार से सुविधाओं की मांग करेंगे तभी जवाबदेही तय होगी. ग़रीब, ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपेक्षा की है इसलिए हम बीमा ख़रीदकर इसकी कीमत चुका रहे हैं.
हां, मैं दुर्घटना बीमा जैसी चीज़ का समर्थन करता हूं. ख़ासकर इस दौर में बड़े शहर में रहने वालों के लिए दुर्घटना का सामना करने की संभावना काफी अधिक है. और दुर्घटना बीमा बहुत सस्ता भी है.
हर साल बजट के मौसम में स्वास्थ्य पर होने वाले ख़र्च को लेकर बहुत हो-हल्ला होता है. मान लीजिए अगर स्वास्थ्य पर बजट बढ़ा दिया जाए तो वे कौन से तीन बिन्दु होंगे जिनसे इन पैसों का उचित इस्तेमाल किया जा सकता है?
मेरे ख्याल से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मज़बूत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. जैसे, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की पहल एक अच्छा आइडिया है. बशर्ते की उसे सही से लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सेंटरों पर स्वास्थ्य सेवक और ज़रूरी दवाइयां उपलब्ध हों.
अभी जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र मौजूद हैं, जहां आमतौर पर एक सहायक नर्स या दाई होती है, वहां एक और नर्स या दाई या कोई पुरुष नर्स की नियुक्ति की जा सकती है. इसके साथ ही मध्यम दर्जे के एक स्वास्थ्य सेवक का भी वहां होना बहुत ज़रूरी है जो कम से कम प्राथमिक स्तर पर मरीज़ की जांच कर उसका इलाज कर सके. ये काम आयुष चिकित्सक भी कर सकते हैं.
वैसे भी, एनएसएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक असल में 95 फ़ीसदी आयुष चिकित्सक एलोपैथी में इलाज करते हैं. ख़ैर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मज़बूत करने के इस उपाए में बजट का 60 से 65 फीसदी ख़र्च होगा. हमने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए ये कैलकुलेशन पहले से ही कर रखा है.
दूसरा नंबर हैं ज़िला अस्पतालों का जिनकी हालत में सुधार बहुत आवश्यक है. दरअसल, ज़िला अस्पताल पर स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे ज़्यादा बोझ होता है क्योंकि यहां छोटे-मोटे इलाज से लेकर बड़ी-बड़ी सर्जरी तक की जाती हैं, जहां मरीज़ अस्पताल में भर्ती होकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करते है.
इसमें सुधार के लिए सभी ज़िला अस्पतालों को कॉलेज-अस्पताल में तब्दील कर देना चाहिए. लेकिन ये काम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए नहीं बल्कि सीधे सरकारी हस्तक्षेप के ज़रिए होना चाहिए. अगर, ऐसा किया जाता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर इलाज का भार बहुत कम हो जाएगा. यहां तक की एक अच्छा उप-स्वास्थ्य केन्द्र मरीज़ के लिए मिडिल अस्पताल की तरह काम कर सकता है. जहां ज़रूरत के अनुसार एक-दो दिन भर्ती होकर मरीज़ ठीक हो सकते हैं और उन्हें ज़िला अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी.
इसके अलावा एक और तरह की स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जिनमें ऐसे डॉक्टरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया जा सकता है जो लोगों को अस्पताल से बाहर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें. शहरी इलाकों में यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है, क्योंकि गांव में तो वैसे भी मध्यम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं. उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में 8000 दांतों के डॉक्टर्स बेरोज़गार थे. सरकार ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब वे मरीज़ को अस्पताल ले जाने की जगह उनकी जांच कर इलाज कर सकते हैं. इससे अस्पतालों पर बोझ कम होगा, और वही मरीज़ अस्पताल में भर्ती होगा जिसे उसकी सख़्त ज़रूरत है. बाकियों का इलाज ये मध्यम स्तर पर उपलब्ध डॉक्टर्स कर सकते हैं.
आपके अनुसार सरकार को स्वास्थ्य पर कितना फ़ीसदी ख़र्च करना चाहिए?
सरकार का कहना है कि वह जीडीपी का 1.6-1.8 फ़ीसदी स्वास्थ्य पर ख़र्च करते हैं. लेकिन, सच यह है कि इसमें वो ख़र्च भी शामिल कर दिए गए हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं- जैसे, पीने के पानी का ख़र्च. डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन जलशक्ति मंत्रालय के अधीन आता है जिसका काम है लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का काम नहीं है. इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और सेंट्रल गर्वमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) को भी इस ख़र्च से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि ये स्कीम आम जनता के लिए नहीं हैं. अगर, इन सभी को बाहर निकाल दें तो असल में स्वास्थ्य पर तो सिर्फ़ 0.8 फीसदी ही ख़र्च हो रहा है.
अगर, सरकार असल में ‘सभी के लिए समान स्वास्थ्य’ के नारे का सम्मान करना चाहती है तो उसे कम से कम जीडीपी का 2.5 फीसदी स्वास्थ्य पर ख़र्च करना चाहिए. तभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के वादों के पूरा किया जा सकता है. अभी तो ज़रूरत यह है कि इसे एक बार में खर्च कर ही देना चाहिए, पांच साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए.