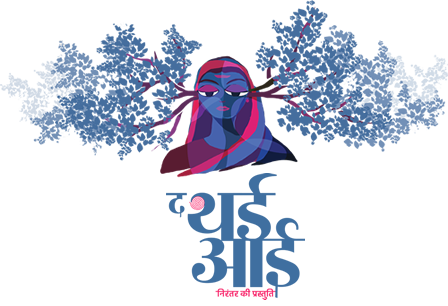एक क्लास असाइनमेंट के तहत मैंने स्टूडेंट्स को एकांतवास (अकेले रहने) या फिर सीमाओं के भीतर रहने के पहलुओं पर सोचने को कहा. लेकिन शर्त यह थी कि वे अपने नहीं किसी और के अनुभवों के ज़रिए इस पर विचार करें. घर में बंद रहने के एकांत को हम किन अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं? इन पहलुओं को कैसे कल्पित किया जा सकता है और उन्हें दर्शाया जा सकता है? आप किसके अनुभवों को दर्शाएंगे और क्यों?
सच कहूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी क्लास में आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपनी मांओं को अपनी छवियों का केंद्र बनाया.
हर्षिता
हर्षिता (जो समाजशास्त्र की पढ़ाई के आख़िरी वर्ष में हैं) कहती हैं “मैं एक अरसे बाद घर पर रह रही हूं और मम्मी को अच्छे खासे बड़े हो चुके लोगों की देखभाल करते हुए देख रही हूं. स्कूल के दिनों में उनका इस तरह हमारा लालन-पालन करना स्वाभाविक लगता था. लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं और मम्मी अब भी हमारी देखरेख में लगी रहती हैं. अब इस पहलू पर मेरा नज़रिया बदल-सा गया है.”
हर्षिता ने उन पलों को कैमरे में क़ैद किया है जो अक्सर हमारी नज़र में नहीं आते, कैमरा पर रिकॉर्ड होना तो बहुत दूर की बात है. उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फ़िल्माया है, कुछ ऐसे पल जो हमें हर्षिता की मां की झलक देते हैं, और कुछ हर्षिता की भी.
“बड़ी अजीब बात है कि इतने बालिग़ हो चुके लोगों की – मेरे पापा तक की – इतनी देखरेख करनी पड़ती है या कहूं कि उन्हें इस देखरेख की ज़रूरत पड़ती है. मज़े की बात यह है कि मम्मी हम सबकी देखरेख करती भी हैं और बड़ी सहजता से. हम सबके लिए इतना सारा काम करते हुए कभी वे इस बात को जताती नहीं हैं. मैं चाहती थी कि इस फ़िल्म में मम्मी का मूल अस्तित्व उभर कर आए.”
“अपनी इच्छा की चीज़ें न करने को लेकर, मैंने हमेशा मम्मी को डांटा है. वे बेहतर अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहती थीं, वे एम.बी.ए करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया. मुझे तो लगता था वे बस बैठ कर मज़े ले रही हैं जबकि “पापा मेहनत से सारे पैसे कमा रहे हैं”. अब मुझे एहसास होता है कि यह बात कितनी बेतुकी है, और मेरी सोच कितनी ग़ैर ज़िम्मेदार.”
हम क्लास में अक्सर ‘प्लॉट’ (कहानी में घटनाक्रम) के बारे में चर्चा करते हुए सोचते थे कि क्या प्लॉट के बग़ैर भी कहानी कही जा सकती है? और कैसे? हम ‘प्लॉट’ या कहानी ढूंढते हैं, बस ऐसी ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो ‘खास’ हों, साधारण नहीं.
स्कूल के शुरुआती दौर से ही, हमें अपनी दुनिया को चंद टॉपिक्स के ज़रिए समझने और व्यक्त करने को कहा जाता है – ‘फलां जगह पर मेरा पहला दिन…’ , ‘क्या समाज में ऐसा या वैसा होनी चाहिए…’ , ‘मेरा फ़ेवरेट…’ , ‘महात्मा गांधी’! गूगल सर्च कर लीजिए, आपको ढेरों ऐसे ‘टॉप टॉपिक्स एंड आयडियाज़ फॉर यूथ’ (यूथ के लिए सबसे प्रमुख विषय और विचार) मिलेंगे जो परिपाटी से चले आ रहे हैं। 70 के ऊपर हो चुके मेरे पापा को भी उनके स्कूली दिनों में यही गिने चुने टॉपिक दिए जाते थे.
लेकिन ज़िंदगी इन टॉपिक्स से कहीं ज़्यादा जटिल और पेचीदा है. हमारी समझ, हमारे रिश्ते, टेढ़े-मेढ़े, घुमावदार रास्तों से गुज़र कर बनते हैं. ऐसे में यथार्थ को सजा धजा कर किसी चमकीले, असाधारण प्लॉट के लिबास में ढाल देना थोड़ा घिसापिटा-सा लगता है. जैसे यही एक फॉर्मूला है ज़िंदगी को मायने देने का. लेकिन रोज़मर्रा के साधारणपन को अपनी नज़र से उजागर करना मुश्किल काम है – इसके लिए हमें अपनी निजी जिज्ञासाओं का सामना करना पड़ता है. कुछ ऐसे मूल सवालों से रू-ब-रू होना पड़ता है, जिनके अक्सर रटे रटाए जवाब होते हैं हमें ये दिलासा देने के लिए कि दुनिया जैसी थी, अभी भी वैसी ही है और हमेशा रहेगी. गौर से चीज़ों को देखने-परखने के लिए हौसला चाहिए, और संवेदना भी. क्या हम पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ अपने आप से और अपने संदर्भ से उलझने की इच्छा रखते हैं?

पिछले साल जब सारी दुनिया लॉकडाउन में कैद थी, हम सब ने खुद को, अपने परिवेश को नए मायने, नए नज़रियों से देखने की ज़रूरत महसूस की. उम्मीद यह थी कि एक साथ हम और भी दृढ़ बन सकेंगे. हर्षिता वापस चेन्नई गई, एक लंबे अंतराल के बाद फिर अपने मम्मी-पापा के साथ रहने.
“अपना काम खुद करने को लेकर पापा के साथ मेरी कई बातें हुईं. अगर उन्हें चाय भी चाहिए, तो वे ख़ुद नहीं बनाते. मम्मी से कहते हैं या मुझसे या मेरी बहन से. चाय बनाना कैसे मेरे काम और पढ़ाई के आड़े आता है, ये उन्हें दिखाई नहीं देता. मैं किसी काम में खोई होती हूं और अचानक उनका आदेश आता है – “ज़रा ये कर दो?” और अब मैं देख पा रही हूं कि कैसे पापा का यह बर्ताव, मम्मी को उनके पसंद की चीज़ें करने से रोकता है.”
“हमेशा किसी और का वक़्त और कार्यक्रम आपके मन में होता है. ख़ुद के लिए समय निकालते हुए आपको और सभी के वक़्त के बारे में सोचना पड़ता है. ऐसे में, मुझे लगता है अपनी इच्छा की चीज़ें न कर पाने की वजह मम्मी की अपनी लापरवाही बिल्कुल नहीं है.”
हम अक्सर औरतों पर सामाजिक प्रजनन (सोशल रीप्रडक्शन) के बोझ की बात करते हैं – कि कैसे इस पहलू को पूरी तरह नज़रंदाज़ किया जाता है. कैसे घर के भीतर जो देखरेख का काम औरतें करती हैं उसे ‘काम’ की तरह स्वीकार नहीं किया जाता, और कैसे परंपरा और रीति-रिवाजों के भूत हम पर मंड़राते रहते हैं. हर्षिता समझने लगती है कि उसके पापा – “… स्वाभाविक रूप से स्त्री विरोधी नहीं हैं. उनका व्यवहार और उनकी सोच सामाजिक परिपाटी से, परवरिश से और आस-पास की प्रचलित मान्यताओं से जकड़ी हुई है.”
जिसे हम “सामान्य” समझ कर स्वीकारते हैं उसके बीज दरअसल गहरे धंसे हुए हैं.
“पापा के भीतर ये सब अचेत रूप से समा गया है” हर्षिता का यह कहना, सटीक सुनाई पड़ता है.
“पापा यह नहीं देख पाते हैं… आख़िर उनके अपने माता-पिता का रहन-सहन, सोचने का तरीका ऐसा ही था. ये अजीब बात है कि रिश्तों पर और आचरण के तरीकों पर पापा मुझसे सलाह-मशवरा कर पाते हैं, लेकिन अपनी बीवी से खुलकर चर्चा नहीं कर पाते.”
“पापा बेहद उखड़ गए जब मैंने उनसे कहा कि मम्मी के प्रति उनका बर्ताव ठीक नहीं है. वे बोले ‘तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हारी मम्मी को कितना कुछ करने की अनुमति दी है.” और मैंने कहा – बस! यही तो दिक़्क़त है. कोई मान कर चले कि उनका आचरण बिल्कुल उचित और निष्पक्ष है, तो उनको यह समझाना बहुत मुश्किल होता है कि शायद वे इतने सही नहीं हैं जितना खुद को समझते हैं. और फिर मम्मी भी तो इन बातों को लेकर काफ़ी अनिश्चित रहती हैं…”
फ़िल्म करने की प्रक्रिया में, कैमरे के देखने वाली नज़र अपने आप सामने आ जाती है. आप जो रेकोर्ड करते या खींचते हैं, वे क्यों करते हैं? आप अपने शॉट को कैसे फ़्रेम करते हैं? फ़्रेम में कौन-सी चीज़ें प्रमुख स्थान पाती हैं और कौन-सी पृष्ठभूमि पर रखी जाती हैं? अगर आप जागरूक और सचेत रहें, तो यह प्रक्रिया काफ़ी गंभीर और वेदना से भरी लग सकती है, लेकिन आख़िरकार आपको आत्मानुभूति की ऊर्जा भी देती है.
जब हमनें हर्षिता की फ़िल्म क्लास में देखी तो सबको ऐसा लगा कि हम “कुछ कुछ… थोड़ा बहुत” उसकी मां को पहचानते हैं. जो छोटी-छोटी डायलोग और साधारण से हाव भाव हर्षिता ने फ़िल्माए हैं, वे उनकी मां के स्वभाव को गहरे और आत्मीय ढंग से रेखांकित करते हैं. शायद इसलिए भी हम सबको यह महसूस हुआ कि हम इस ‘मां’ को जानते और समझते हैं. हर्षिता का अपनी मां से रिश्ता हम समझ पाते हैं. मां के मूल अस्तित्व को दर्शाने की हर्षिता की चाहत, हमें भी महसूस होती है. उस पल हमें हर्षिता की मां में अपनी माओं की छवि नज़र आने लगती है.
वक़्त के साथ, हर्षिता मानती हैं कि घर में सत्ता का संतुलन बदल रहा है. “अब मैं और मेरी बहन बड़े हो चुके हैं और मम्मी हमें अपने निर्णय खुद लेते हुए देखती हैं. इससे उनकी अपनी स्वतंत्रता को लेकर सोच भी प्रभावित हुई है. मैं समाजशास्त्र की पढ़ाई कर रही हूं और अपने सब्जेक्ट के कुछ प्रमुख विचारों को घर में रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा भी बनाती हूं मेरी मम्मी…” कहते-कहते हर्षिता रुकती हैं, उनकी आंखें चमकने लगतीं हैं और एक विचार उनके मन में उभरता है – “… पिछले दिनों, एक बार पापा मम्मी को कोई ऐसी बात समझा रहे थे जो उन्हें पहले से पता थी, तो मम्मी ने उनसे कहा – ‘देखो, मेरे साथ मैनस्प्लेनिंग * मत करो!’ उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा – “मैंने सही कहा न, हर्षिता?”
*यह अंग्रेज़ी शब्द का सृजनात्मक जोड़ है – मैन यानी पुरुष और स्प्लेनिंग यानी समझाना. मैनस्प्लेनिंग पुरुषों की उस प्रवित्ति को जन्म देता है जहां उन्हें लगातार औरतों को समझाने और खुद को जानकारी, अनुभव और ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने की ज़रूरत महसूस होती है.
प्रतुल
“मैं अपने शॉट्स के ज़रिए, ये दर्शाना चाहता था कि कैसे मेरी मां, हमारे जीवन में, सब कुछ समेटकर संजोकर रखती हैं. अगर वे नहीं होतीं तो सब कुछ बिखर जाता… उन्होंने हमें महसूस कराया कि ज़्यादा कुछ बदला नहीं है.”
प्रतुल यूनिवर्सिटी में ‘इतिहास और अंतरराष्ट्रीय संबंध’ की पढ़ाई के दूसरे साल में है और फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते लखनऊ में अपने घर पर रह रहे हैं. पहली नज़र में, प्रतुल के शॉट्स हमें सिनेमा की दृष्टि से कुछ ख़ास नहीं लगे. ख़ास थी तो उनकी अपने मुख्य पात्र को लेकर एकाग्रता और निश्चय.
“मैं ११वीं कक्षा में था जब मां ने अपना कारोबार शुरू किया. तब उन्हें नहीं लगा था कि ये उनकी और हमारी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा.”
नवंबर 2019 में प्रतुल की ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया, जिसका उसे अंदेशा नहीं था. “पापा को किड्नी की बीमारी हुई. उनकी दोनों किड्नी फ़ेल हो गईं. पहले वे काम करते थे, पर अब उन्हें घर पर रहना पड़ रहा है. जनवरी 2020 प्रतुल के परिवार को पता चला कि प्रतुल को ग्लॉकोमा है. उनकी बाईं आंख की रोशनी 80% और दाईं आंख की 45-50% है. प्रतुल कहते हैं कि “मैं मैनेज कर रहा हूं… इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है.”
प्रतुल जब अपनी मां को फ़िल्माते हैं, तो उन दृश्यों में भी वही निश्चय और स्पष्टता नज़र आती है जो उनकी बातों में झलकती है. मुख्यधारा की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों में, कठिन परिस्थितियों से जूझते किरदारों को दर्शाकर, उनके प्रति सहानुभूति पैदा करना आम बात है. लेकिन प्रतुल की फ़िल्म में मां में किसी प्रकार की लाचारी या ट्रेजडी नहीं है. फ़्रेम में मां है. मां ख़ुद फ़्रेम है. इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है.
जब कोई चीज़ पूरी तरह आपके फ़्रेम पर हावी हो और हमेशा उसका केंद्र बना रहे, तो लाज़मी है कि आप इस फ़्रेमिंग के पीछे के अर्थ और भाव को समझना चाहेंगे. कौन है यह औरत? मैं उसे रोज़ाना के छोटे-बड़े काम करते हुए क्यों देख रही हूं? उसकी कहानी क्या है? प्रतुल के शॉट्स में मां मात्र विषय-वस्तु नहीं है जिसे आप दूर से किसी प्रदर्शनी की तरह देख सकें. वे न ही कोई असाधारण हीरो हैं और न ही लाचार पीड़िता. प्रतुल के कसे हुए फ़्रेम्ज़ में वो नज़दीकी है जो आपको छोटी से छोटी चीज़ों पर ग़ौर करने और उनमें छिपे अर्थों को खोजने पर मजबूर करती है.
“कपड़ों को लेकर हमेशा से उनमें एक हुनर था… सिलाई करने की रुचि उनमें हमेशा रही है. मैं 7वीं कक्षा में था जब उन्होंने व्यापार शुरू किया. व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मां कई सारे ब्लॉग्स पढ़ने लगीं. फिर उन्हें कुछ फ़ेसबुक ग्रूप्स मिले जहां लोग एक-दूसरे के साथ साझेदारी बनाकर अपने सामानों की ख़रीड-फ़रोख्त करते हैं. मां उन वाट्सऐप ग्रूप्स का भी हिस्सा बनीं जो आपका सम्पर्क ऑनलाइन मार्केट के सप्लाइअर्ज़ और विक्रेताओं से कराते हैं. वक़्त के साथ व्यापार फैलता गया. कारोबार को लेकर उनकी समझ भी स्पष्ट होती गई.”
प्रतुल को लगता है कि मां को हमेशा कठिन निर्णय लेने पड़े हैं. शादी के पहले, वे एक बैंक में कैशियर थीं, लेकिन प्रतुल के पैदा होते ही उन्होंने यह काम छोड़ दिया. “वे मुझे पाल कर बड़ा करना चाहती थीं”, ऐसा वे कहती हैं. उनकी एक जूनियर सहकर्मी आज एच.डी.एफ.सी बैंक में मैनेजर है. मां भी अपने काम में सक्षम थीं, आज वो भी किसी बड़े पद पर होतीं. लेकिन मुझे पालने-पोसने के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया.”
आज भी स्थिति कुछ आसान नहीं है. “वे हमेशा डेडलाईन पर होती हैं, ग्राहकों का काम समय पर पूरा करने में लगी रहती हैं. आप समझ सकती हैं. आप भी तो एक प्रोफ़ेशनल हैं.” जिस स्पष्टता से प्रतुल अपनी मां और उनकी परिस्थिति के बारे में बताते हैं, उसमें उनकी समझ गूढ़ रूप से झलकती है.
“एक बात मुझे साफ़ नज़र आती है कि वे कभी किसी (ग्राहक/सप्लायर्ज)को हमारे घर की समस्या नहीं बता पातीं – वे तय समय से अधिक वक़्त नहीं मांग सकतीं या ये नहीं कह सकतीं कि अभी वो कॉल्ज़ लेने की स्थिति में नहीं हैं. लेकिन घर की परिस्थिति तो हमेशा नाज़ुक रहती है, हर घंटे कुछ न कुछ बदलता रहता है. पापा भले अभी ठीक महसूस कर रहे हों, लेकिन दो घंटे में ही उनकी तबीयत बिगड़ सकती है. उन्हें लेट कर आराम करना पड़ सकता है… उन्हें कष्ट होता है. ऐसे में मां को उनकी देखभाल करनी ही पड़ती है. ऐसे में किसी क्लाइयंट का कॉल आ गया तो वे यह भी नहीं कह सकतीं कि अभी वो अपने पति की… या मेरी… देखरेख में व्यस्त हैं.”
“उन्हें अपनी भावनाओं को परे हटाकर वो कॉल लेना पड़ता है. क्योंकि प्रोफ़ेशनल दुनिया में कोई इन बातों को नहीं समझता. वे पापा का डायऐलिसस कराने भी जाएं, तो उन्हें वेटिंग रूम में बैठकर कॉल पर कॉल लेने पड़ते हैं. वे यह भी नहीं कह सकतीं कि अभी 6 घंटों के लिए बाहर हैं… और क्लाइयंट से रात में ही बात कर पाएंगी. प्रोफ़ेशनल काम भावुक होकर नहीं होता. ये एक बड़ी चुनौती है जिससे उन्हें लगातार जूझना पड़ता है. इस तरह उनके घर और काम की दुनिया आपस में उलझ जाती है.
किसी एहसास को कैमरे में कैसे कैद किया जाता है? अपनी मां, और घरेलू परिस्थिति के बारे में जो प्रतुल अपने शब्दों में ज़ाहिर करते हैं, वो उनके शॉट्स में इतने साफ़ तौर पर नहीं दिखता. डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में हमें अक्सर ऐसे ‘इंटरव्यू’ (साक्षात्कार) मिलते हैं जहां किरदार हमें उनके रोज़ाना संघर्ष के बारे में ख़ुद बता देते हैं, लेकिन प्रतुल इस तकनीक का सहारा नहीं लेते. प्रतुल के शॉट्स में वो ‘सेल्फ़-रिफ्लेक्टिव’ शॉट्स भी नहीं हैं जहां फ़िल्मकार ख़ुद अपने भाव और सोच व्यक्त करने लगते हैं (उनकी आवाज़ किसी भी चित्र पर चिपका दी जाती है – जैसे दीवार पर परछाई, पत्तों से बिखर कर आती धूप, पानी पर बनती तरंगें वगैरह – जो कहीं भी फ़िट हो जाती हैं और जिनका अपना कोई ख़ास अर्थ नहीं होता – सिवाए इसके की कहानी को गति बढ़ाने में मदद करे.
आज के दौर में चित्र और चित्रण को लेकर हमारी धारणाएं सोशल मीडिया से इतनी प्रभावित हैं कि दृश्यों में समय की अनुभूति कम से कम होती जा रही है.
दृश्य गढ़ते वक़्त हम बेचैन रहते हैं. एक दृश्य से दूसरे दृश्य की ओर भागते रहते हैं – मानो कुछ छूट रहा है. हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर हम किसी दृश्य पर ज़्यादा देर ठहरे, तो कहीं दर्शक बोर न हो जाएं. अगर कहीं वे इधर-उधर देखने लगें तो? फ़िल्म करते वक़्त, शॉट्स में समय की अवधि का बोध – इस विषय पर क्लास में विचार करना मुझे हमेशा कठिन मालूम पड़ता है.
क्योंकि यह विचार है ही इतना अमूर्त. किसी शॉट को कहां पर कट करना है ये कैसे पता चलता है?
प्रतुल की फ़िल्म का हर शॉट एक मिनट से थोड़ा लम्बा है. इसके बावजूद, क्लास में फ़िल्म देखते वक़्त हमें बोरियत नहीं महसूस होती. एक अनुभूति पैदा होती है, भले ही उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो. बल्कि प्रतुल के शॉट्स जब एकाएक कट होकर दूसरे शॉट की ओर बढ़ते हैं, तो हमें एक अधूरापन महसूस होता है. हम उन दृश्यों को और थोड़ी देर तक देखना चाहते हैं.
प्रतुल के लंबे शॉट्स दृश्यों के प्रत्यक्ष अर्थ के अलावा, हमारी कल्पना से बने मायनों को भी उभरने का समय देते हैं. (जैसे पहले शॉट में, अगर मां के घर से बाहर निकलने के बाद भी शॉट चलता रहता, तो क्या हम बैकग्राउंड की आवाज़ों के ज़रिए घर के बाहर और भीतर की दुनिया का रिश्ता किसी अलग ढंग से समझ पाते? जब मां खाना बना रही हैं, तो उस क्षण को ज़रूरत से अधिक ठहर कर देखें, तो क्या मायने बनेंगे? कैमरा को रोके बिना समय का विस्तार करने पर क्या कुछ हो सकता है? क्लास में सभी को अपनी अलग संभावना कल्पित करने का मौक़ा मिलता है.)
प्रतुल के शॉट्स अचानक ज़रूर कट हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके फ़िल्म के दृश्यों की अवधि क्लास के दूसरे फ़िल्मों से लम्बी है. शायद अपने भीतर, और अपने घर की परिस्थिति में प्रतुल इसी तरह समय का अनुभव करते हैं. शायद प्रतुल के लिए समय के मायने उनका अनुभव खुद के भीतर, अपने घर के भीतर इस तरह का लंबा खिंचा हुआ-सा ही है.
महक
“जहां तक मैं याद कर पाती हूं, मम्मी ने हमेशा ख़ुद को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखा है. वे हमारे परिवार में सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, और हम हमेशा से चाहते थे कि वो ‘फ़ूड इंडस्ट्री’ (खाने से संबंधित किसी व्यवसाय) में काम करें. वे इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेती थीं. लेकिन जनवरी में, वे खाने से संबंधित कई वाट्सऐप ग्रूप्स में शामिल हुईं. वे खाना बनाने और खाने के इर्द-गिर्द बने सामूहिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगीं. फिर लॉकडाउन के बाद, उन्होंने इसको अपना कारोबार बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया. उन्होंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, एक मेन्यू तैयार किया और ऑर्डर लेने लगीं. अभी तक जो भी काम उन्होंने किए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा वे इस काम को लेकर उत्साहित थीं.”
महक ‘अर्थशास्त्र और ललित कला’ की पढ़ाई के दूसरे साल में हैं. हर्षिता और प्रतुल की तरह, वे भी लॉकडाउन के चलते अपने घर मुंबई में रह रही हैं. महक मुझे बताती हैं कि कैसे उनकी मां ने कई सारे व्यवसायों में अपना हाथ आज़माया, लेकिन घर और काम के बीच तनाव के चलते उन्हें काम छोड़ने पड़े. उन्हें काम करने में मज़ा आता, वे आत्मनिर्भर भी महसूस करतीं, लेकिन “… उन्हें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े. ख़ासकर हमारी देखभाल के लिए” महक कहती हैं.
प्रतुल की तरह, महक भी ठहराव और आत्मीयता के साथ अपनी मां को फ़िल्माती हैं. उनका शॉट लगभग चार मिनट से भी लंबा है. यह “पहली बार” हुआ है कि वे घर पर इतने लंबे समय तक रह रही हैं. पहली बार उन्होंने “ग़ौर से देखा” अपनी मां को काम करते हुए. इस ग़ौर से देखने को वे अपने शॉट्स में मानो हु-ब-हू तब्दील करती हैं. जो वे देख रही हैं, चाहती हैं कि हम भी देखें – वे श्रम और मार्मिकता जो उनकी मां के खाना बनाने की प्रक्रिया में झलकती है.
महक अपनी मां के हाथों की फुर्ती, अपनी फ़िल्म की गति और लय के ज़रिए बड़े सूक्ष्म रूप से दर्शाती हैं (किचन से बादाम लेकर आती हैं, बादाम फ़्रेम के फ़ोकस में रह जाते हैं, और महक वापस मां के पास किचन में चली जाती हैं – इस विधा में चीज़ों को दर्शाना, महक के लिए ज़रूरी है. वे चाहती हैं दर्शक भी इसे महसूस करें.) कैमरा के फ़्रेम के बाहर हो रहे संवाद भी हमें उन पलों से जोड़ते हैं.
“हर दिन डिनर के बाद, मैं मम्मी के साथ बैठती हूं और वे कुछ नया बनाने की कोशिश करती हैं. पकवान के आकार पर प्रयोग करती हैं, उसकी रूपरेखा संवारती हैं – जैसाकि मैंने अपने शॉट में दिखाया है. रेसिपी में क्या सही बैठ रहा है इस पर काम करती हैं, कुछ नया बनाती हैं और मुझे बुलाकर टेस्ट करने को कहती हैं – ‘कैसा लगा?’ इन पलों के ज़रिए हमें एक-दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है.”
महक मानती हैं कि उनके अपने निर्णय उनकी मां से अलग होंगे. “आज भी जब मैं मम्मी से कहती हूं कि मुझे मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना है, जिसमें अक्सर दूसरी जगहों का दौरा करना पड़ता है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है – ‘तो फिर घर कैसे संभालोगी?’ लेकिन मेरे और मेरी बहन के लिए, ये चीज़ें बहुत साफ़ हैं. घर संभालने के लिए हम किसी को काम पर रख सकते हैं या कोई और तरीक़ा निकाल सकते हैं. लेकिन अपनी इच्छा का हर काम करने से पहले ये सोचना कि घर कौन संभालेगा – ऐसा तो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये तो नहीं कि घर मेरे लिए ज़रूरी नहीं है.”
इन मतभेदों के बावजूद, महक को लगता है कि उनकी मां के काम करने से, कुछ ऐसी नई संभावनाएं पैदा होती हैं, जो पहले मुमकिन नहीं थीं. “ठीक-ठीक मैं भी नहीं कह सकती, लेकिन उनके काम करने से, मेरे और पापा के बीच भी राजनीतिक चर्चा करने का स्पेस बनता है… सभ्य क़िस्म की राजनीतिक चर्चा.”
महक याद करती हैं कि कैसे “एन.आर.सी और सी.ए.ए के दिनों में” उनकी और उनके पापा की किसी भी बात पर नहीं बनती थी. “मेरे पापा ने एक बार मुझसे कहा कि अगर आज तुम्हारे दादा ज़िंदा होते तो इस विषय पर तुम्हारी सहानुभूति देखकर तुम्हें परिवार से बाहर निकाल देते. उस दिन के बाद हमने तय किया कि अगर पापा-बेटी का ये रिश्ता हमें बरक़रार रखना है तो हमें राजनीति पर बहस बंद करनी होगी. लेकिन आज जब हम सब मम्मी के काम पर चर्चा करते हैं, तो विषयों का विस्तार अपने आप बड़ा हो जाता है और हम कई मुद्दों पर एक-दूसरे से बात कर पाते हैं.”

ये कैसे मुमकिन हो पाया? शायद इसलिए कि खाना अपने आप में एक राजनीतिक विषय है – खाने में क्या डलता है? कौन क्या और कैसे खाता है? – शायद इसके चलते इन मुद्दों पर बात हो ही जाती है. सामान्य सुशील-सी बातें, जिनके ज़रिए हमारे पूर्वग्रह और हमारी उदारता दोनों उभर कर आते हैं और शायद हमें उन्हें समझने का मौक़ा भी मिलता है? “शायद. कारण जो भी हो, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है.”
बल्कि कई स्त्रीवादी शिक्षकों ने, ख़ास तौर पर खाने को केंद्र में रखकर शरीर और यौनिकता पर चर्चाएं चलाई हैं. ‘निरंतर’ संस्था द्वारा हिंदी में प्रकाशित ‘खुलती परतें: यौनिकता और हम’ जिसकी संरचना कई स्त्री समूहों के साथ वर्क्शाप के ज़रिए हुई, इसका एक प्रमुख उदाहरण है. इस प्रकाशन में, खाने के प्रतीकों के ज़रिए, यौनिक व्यवहार को लेकर हमारी जानकारी, चुनाव, पसंद-नापसंद, और शुद्ध-अशुद्ध की धारणाओं पर चिंतन किया गया है.
जितनी विभिन्न हमारी प्रेम और यौनिकता को लेकर चाहतें हैं, उतने ही विभिन्न प्रकार के टेस्ट हमें खाने की दुनिया में मिलते हैं. जिस तरह कुछ लोग मांसाहारी खाने की बजाए शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, वैसे ही हमारी यौनिकता को लेकर भी अपनी अपनी पसंद होती है. जिस प्रकार समय के साथ खाने में हमारा टेस्ट चेंज हो सकता है, वैसा ही हमारी यौनिकता को लेकर भी हो सकता है. हम क्या और क्यों खाते हैं – ये सवाल हमारी सामाजिक परिपाटी से जुड़ा होता है. इसी तरह हमारी यौनिकता भी सामाजिक अनुकूलन का ही हिस्सा होती है.
खाने की दुनिया में अपनी मां के सफ़र के बारे में बताते हुए महक की आंखें चमक उठती हैं. उन्हें एहसास होता है कि कैसे मां के काम करने की वजह से उनके परिवार में नज़दीकियां बढ़ी हैं. इसका कोई सीधा संबंध भले नज़र न आता हो, लेकिन भीतर कहीं इस बात का एहसास सच्चा मालूम होता है. घर के हर छोटे बड़े विवरण पर ग़ौर देकर अपनी मां को फिल्माते हुए महक इसी एहसास को अपने शॉट्स में कैद करने की कोशिश करती है. इस पर तुम्हें एक पूरी फ़िल्म बनानी चाहिए, मैं कहती हूं. हम हंसते हैं. शायद कभी ऐसा हो….
इस लेख का अनुवाद प्रशांत पर्वत्नेनी ने किया है.