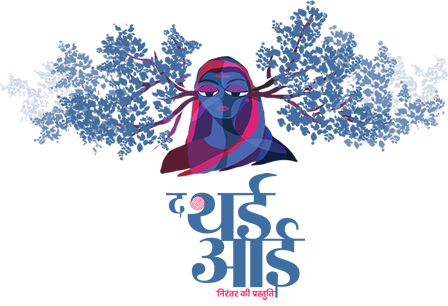यह हमारे ‘मज़ा और खतरा’ संस्करण के भीतर ‘अवचेतन और यौनिकता’ लेख शृंखला में प्रकाशित दूसरा लेख है. यह संबंधित विषय पर लेखक के शोध, उनके विचार और विश्लेषण पर आधारित है. यह लेख शृंखला मूल अवधारणाओं को सामने लाने का प्रयास करती है और सीखने-सिखाने के तरीकों को भी उभारने का काम करती है.
जया शर्मा ‘मज़ा और खतरा’ संस्करण की अतिथि संपादक हैं.
मेरे लिए दिलो-दिमाग या अवचेतन (गाफिल), ये उन सारी हकीकतों का एक दायरा है, जिसे सीधे-सीधे न महसूस किया जा सकता है, न सोचा जा सकता है. इसे सीधे सुना, देखा या छुआ भी नहीं जा सकता. फिर भी यह एक ज़ोर है, जो बहुत ही ताकतवर है और जो निरंतर हर उस चीज़ पर असर करता है जिसे हम महसूस करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं. यह हर जगह लागू होता है – हम क्या खाना पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, परिवार से हमारा रिश्ता कैसा है, हम कैसा साथी चुनते हैं या हम किस राजनैतिक नेता को चुनते हैं.
हमारा अवचेतन एक गोदाम की तरह है जहां ज़िंदगी में हमने जो कुछ भी अनुभव किया, उन सभी के निशान इकट्ठा होते रहते हैं. असल में तो हर वो अनुभव, जो कोख में रहने से अब तक हमने अनुभव किया है, इस गोदाम में जमा होता रहता है. कोई भी तजुर्बा बिना निशान छोड़े गायब नहीं हो जाता.
हमारा अवचेतन हमारे सारे तजुर्बों की निशानियों को बिना कोई धारणा बनाए दर्ज करता रहता है. कुछ भी कांट-छांट नहीं की जाती. कुछ भी सेंसर नहीं किया जाता. कुछ भी भुलाया नहीं जाता.
इन अनुभवों के निशान अवचेतन से चेतन में भी लौट सकते हैं. जैसे, ये कहना कि ‘अरे, ज़बान फिसल गई’ या ऐसे कई काम जो होशो-हवास में किसी तय इरादे से नहीं किए जाते, इन जगहों पर इन्हें देखा-सुना जा सकता है. इसमें सपने और कल्पनाएं भी शामिल हैं. हालांकि, जब अवचेतन में मौजूद निशान चेतन में अपनी मौजूदगी महसूस कराते हैं, तो उन्हें सीधे-सीधे या शाब्दिक अर्थों में नहीं पढ़ा या समझा जा सकता. ये निशान हमारे अवचेतन में दबे रहे हैं, और चेतन में चालाकी और छल अपनाते हुए लौटते हैं. हमारा चेतन मन इनकी सेंसरशिप नहीं कर पाता क्योंकि ये चकमा देने में उस्ताद होते हैं.
हालांकि हम आमतौर पर अवचेतन को बहुत ही निजी या खुद के अनुभव के तौर पर ही लेते हैं, पर एक सामूहिक अवचेतन भी होता है. जैसा कि मेरी पसंदीदा नारीवादी मनोविश्लेषक जैकलीन रोज़ लिखती हैं, “हम दूसरों से आबाद होते हैं.”
हमें लगता है कि जो हम महसूस करते हैं, समझते और सोचते हैं, वही है हमारी निजी और सामूहिक ज़िंदगियों का सच. जो मुझे पता है, वही सब कुछ है, मौजूद है. जो मैं जानबूझकर, इरादतन, लफ़्ज़ों या इशारों से ज़ाहिर कर सकती हूं, वही मायने रखता है.
लेकिन अगर ऐसा होता कि सब कुछ ज़ाहिर किया जा सकता है, सोचा और समझा जा सकता है तो इसके विस्तार में मुझे इतनी हैरानी-परेशानी क्यों होती. इतना कुछ है जो समझ में नहीं आता, जिसे संज्ञानात्मक मन (आलमी ज़हन) से नहीं समझा जा सकता और चाहे मैं कितना भी चाहूं, न लफ़्ज़ों में बयान किया जा सकता है और न इशारों में. इन सबमें अवचेतन (साइकी) इस पूरी पहेली का सूत्र है.
मैं अब आपके साथ ‘प्यार और सेक्स’ पर किए गए एक शोध की चंद बातें साझा करना चाहती हूं. ये शोध अभी तक अप्रकाशित है, और अनाम भी. (वैसे यहां ये एकदम फिट बैठता है क्योंकि हम अचेतन की ही बात कर रहे हैं!) इस शोध के तहत एक अनाम ऑनलाइन सर्वे किया गया था. सर्वे में जवाब देने वालों से उनके रोमांटिक-सेक्सुअल प्यार के अनुभवों के बारे में पूछा गया. साथ ही मैंने उनसे उनकी सबसे उत्तेजक, गोपनीय औऱ गंदी माने जाने वाली फंतासियों या कल्पनाओं को भी बताने के लिए कहा, जो उन्होंने बताईं भी. सभी प्रतिभागियों को ये मालूम था कि उनके द्वारा साझा की गई ये बातें पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि शोध करने वालों को उनका ईमेल आईडी तक भी नहीं पता चलेगा. (सर्वे मंकी वेबसाइट ज़िंदाबाद!).
यह कोई बहुत बड़ा सर्वे नहीं था. इसमें 30 लोगों ने जवाब दिए थे. जवाब देने वालों में सभी शहरी, अंग्रेज़ी बोलने वाले थे. इनमें आधे से ज़्यादा प्रतिभागियों ने खुद को महिला एवं नारीवादी की पहचान से ज़ाहिर किया. इस शोध के दौरान ही, रोमांटिक-सेक्सुअल प्यार को लेकर कुछ गहरे इंटरव्यूज़ भी किए गए थे जिनके लिए कुछ सवाल तो पहले से तय थे बाकि सामने किस तरह की कहानियां हैं उसपर निर्भर थे.
मनोविश्लेषण के विचारकों के चुनिंदा लेखन की साहित्य समीक्षा करने के बाद, मनोविश्लेषण की अवधारणाओं की मदद से सर्वे और इंटरव्यू के जवाबों पर करीब से गौर किया गया था.
मैं चाहूंगी कि उनमें से एक साक्षात्कारकर्ता से आप भी मिलें. उसका नाम है ई*. शोधकर्ता और ई, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन पिछले एक दशक से एक-दूसरे की कोई खोज-खबर नहीं ली थी. कॉलेज के दिनों में एक युवा नारीवादी होने के नाते, इश्क और चाहतों को लेकर उन दोनों के विचार लगभग एक जैसे थे.
और दोस्तों को अपने महबूब जितना ही महत्त्वपूर्ण मानना उनके संघर्ष का नारा था. महबूब से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं.
तो, इतने सालों बाद, जब वे मिले और शोधकर्ता ने उससे कहा कि वो इश्क के बारे में बात करना चाहती है, तो उसने ताना मारते हुए कहा, “क्या तुम मुझसे दोस्ती के बारे में नहीं पूछना चाहती?” मगर वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी उस तरह से आगे नहीं बढ़ी. ई बताती है:
मेरा प्रेमी मेरी ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा (डिफ़ॉल्ट सेटिंग) बन गया. एक ऐसा संबंध जो मुझे असल में ज़िंदा महसूस कराता था. यहां तक कि सबसे करीबी दोस्तों के साथ बिताए गए सबसे खूबसूरत पल भी कुछ हद तक कम सजीले थे. कोई फिल्म देखना और इस बारे में उसे न बताना, ऐसा था, मानों मैंने फिल्म देखी ही नहीं. नई ड्रेस पहनना और उसकी तस्वीर उसे न भेजना, कोई गाना सुनना, और उसे उसका लिंक न भेजना… ऐसा लगता था जैसे कोई हसरत अधूरी रह गई हो.
और उसे जवाब देना ही होगा. उसकी नज़र, चाहे कुछ भी हो, मुझसे हटनी नहीं चाहिए. उस वक्त मुझे भयंकर घबराहट हुई, जब मैंने देखा और पाया कि उसकी नज़र मुझसे हट गई थी. बेशक, ऐसा बहुत बार हुआ था. पर जब भी ऐसा होता, तो मैं बस ऊं…ऊं….कर पड़ती. (यहां वो छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ की नकल करती है जो अपने ऊपर ध्यान दिलवाने की कोशिश करता है) वैसे, मेरा मतलब है, ये सब मैं ऑनलाइन ही करती. अगर इससे काम नहीं बना, तो ऊं..ऊं…आं…ऊं…ऊं…., और अगर उससे भी नहीं बना तो ऊं….ऊं..आं….ऊं…ऊं….ऊं…ऊं…. सोचो, हम यहां एक ऐसी औरत की बात कर रहे हैं जो पचास की होने वाली है!
तो, जब ये मासूमियत, ये दिलकशी काम करना बंद कर देती है या ढलने लगती है, तो चिल्लाना शुरू होता है: ‘मेरे पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं है’, ‘वैसे भी किसे परवाह है’. मेसेज के बाद मेसेज. केवल यह सुनने के लिए कि ‘माफ करना, बॉस आ रहे हैं’, ‘पत्नी बीमार है’, ‘दफ्तर में कोलीग खुदकुशी कर सकता है.’ अक्सर इससे कम में कोई बहाना नहीं होता था, ये समझाने के लिए कि हकीकत कितनी बेरहम है. असल में यहां मुकाबला सिर्फ मेरे प्रेमी के असली या काल्पनिक प्रेमी के साथ नहीं था, बल्कि खुद ज़िंदगी के साथ था. मैं बेचारी! ये ‘कभी पूरी न होने वाली कमी का भाव’ मेरे भीतर से कभी गया ही नहीं.
ई नारीवादी आंदोलन और क्वीयर आंदोलन का हिस्सा रही है. “मैं पॉलीएमरस हूं (सहमति से एक ही वक्त में एक से ज़्यादा रोमाटिंक-सेक्सुअल रिश्तों में रहना). मैं एक नारीवादी हूं जो आशिकों को अपनी निजी बपौती की तरह रखने में यकीन नहीं करती,” वह कहती है. लेकिन जलन की भावना से वो भली भांति परिचित है.
मुझे पूरी तरह से शक था कि उसका लखनऊ की किसी बंदी के साथ, जिसे मैं भी जानती थी, रिश्ता था. वह हमेशा ठीक उसी वक्त ऑनलाइन आता था जब वह आती थी. मैं यह देखने के लिए बार-बार जांच करती थी कि क्या ऐसा हो रहा है! मैं गर्दन घुमाकर देखती तो कभी इसके प्रोफाइल पर जाकर देखती, तो कभी उसके – जैसे टेनिस में विम्बलडन फाइनल का मैच चल रहा हो. वैसे ये उससे कम रोमांचक नहीं था! मैं पूरी शिद्दत से खुद को ये याद दिलाती कि हम एक पॉली रिश्ते में थे, बावजूद इसके, न सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया था बल्कि उसकी ज़िंदगी भी नर्क कर दी थी. वह इसे नकारता रहा और आखिरकार, मुझे पता चल गया कि दोनों के बीच चक्कर चल रहा था.
उसकी हंसी उसके अपने जज़्बातों से बेमेल होने को नहीं छिपा पा रही थी.
मैं खुद को हैरत में डालती, मुझे खुद से घिन आती लेकिन मेरे लिए इस तरह बार-बार जलन की ओर लौटने की चाहत में कुछ नशा सा था. जलन चाहे ख्यालों में हो या असल ज़िंदगी में, ये जिस तरह सामने आती है, उसमें एक स्वाद तो है. इसमें भले ही मुझे कष्ट पहुंचे या इसके लिए तड़पना पड़े. यह ऐसा है जैसे वक्त-वक्त पर मेरे सिस्टम को जलन की एक खुराक की ज़रूरत होती है और मैं पाती हूं कि मैं इसी की तलाश में फिर रही हूं. यह मेरी ज़िंदगी की लानत है. वह चाहत, लत की तरह बार-बार उस जगह पर लौटने की जहां मैं खारिज की जाती हूं और जहां मैं केवल एक दर्शक हूं जो बार-बार प्रेमी के असली या ख्याली प्रेमी/प्रेमियों के फेसबुक पेज की निगरानी रखती है.
ई के साथ इंटरव्यू के दौरान कई तरह के पहलुओं को जाना-समझा, जिनमें से कुछ की झलक मैंने यहां आपके साथ साझा की. वे खासकर रोमांटिक सेक्सुअल प्यार के बारे में थी. पर चाहतें, बिना शक, दोस्ती में भी असर कर सकती हैं. दोस्ती से सेक्सुअलिटी को निकालना बेईमानी होगी, लेकिन क्या रोमांटिक-सेक्सुअल प्यार में कोई खास ज़हनी ऊर्जा होती है?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने मनोविश्लेषक उर्वशी अग्रवाल की ओर रुख किया. उर्वशी अपने एक लेख (ऑफ मदर्स एंड थेरेपिस्ट) में लिखती हैं, “सेक्सुअल या यौनिक तजुर्बे इतने असरदार होते हैं कि वे हमारे सबसे पहले अंतरंग संपर्क की याद दिलाते हैं, जोकि मां के शरीर के साथ होता है.” बेशक, वह यौनिक या सेक्सुअल के बारे में लिख रही हैं, और हमें ये भी पता है कि वो रोमांटिक से अलग हो सकता है औऱ ज़रूरी नहीं कि प्यार से जुड़ा हो (और इसके उलट भी हो सकता है), लेकिन यहां वह एक ज़रूरी विचार की ओर इशारा करती हैं, हमारी पहली अंतरंगता का, और मां से इसके रिश्ते का.
‘मां’ के बजाय हम ‘शुरूआती पालने-पोसने वालों’ के बारे में भी सोच सकते हैं. हालांकि, विषमपितृसत्ता की हकीकत को देखते हुए, हम मां को ही केंद्र में रखते हैं.
हमारी पहली अंतरंगता की याद मां के साथ है, यह भी एक ऐसी अंतरंगता है जो जल्द ही बदलाव से गुज़रती है. वो सुख जो नवजात शिशु कभी अपनी मां के जिस्म से और अपने जिस्म से हासिल कर सकता था, उसपर बंदिश दिखने लगती है. बच्चे के अवचेतन में ये कल्पना है कि मां सिर्फ मेरी है. नवजात से बचपन में जाने का मतलब हकीकत के साथ दीगर सख्त मुलाकातें थीं. यह पता चला कि हमारी मां, आखिरकार, केवल हमारी नहीं थी. उसकी ज़िंदगी में और भी लोग थे और उनकी मांगे भी वो पूरा कर रही थी, खासकर पिता की. इस तरह हमारी ज़िंदगी की पहली फंतासी बेरहमी से कुचल जाती है. मां के साथ होने का जो भ्रम था, वो टूट जाता है. अब से, मां से मिल पाना हमेशा बंदिशों के साथ होगा, चाहे वह दूसरों की हम पर हों, उनपर रखी गई मांगों से हों या उनकी अपनी चाहतों से.
प्यार और खासकर रोमांटिक सेक्सुअल प्यार, इस खोने की भरपाई करने का अहसास पैदा करता है ताकि हमारी अंतरंगता की फंतासी पूरी हो सके. प्यार जैसे हमें उस लम्हे में वापस ले जाता है जो हमारे पैदा होने से पहले था, जब हमारे और हमारी मां के बीच एक भौतिक निरंतरता मौजूद थी. पैदाइश का वह पल, उस वक्त को सामने लाता है, जब हम अलहदा, एक-दूसरे से जुदा वजूद बन जाते हैं. ज़िंदगी का ये सफर बार-बार हमारे ज़ेहन में उभरता है. मगर हम प्यार के ज़रिए, भले ही थोड़े वक्त के लिए, इस जुदाई को तोड़ने और अपने और प्रेमी के बीच निरंतरता खोजने की कोशिश करते हैं.
इसे ही ई ने अपनी ‘एक हो जाने की ख्वाहिश’ से जुड़ी हताशा और नामुमकिन सा अहसास कहा. ज़ाक लाकां का मनोविश्लेषण हमें इस मज़बूत अहसास को कुछ इस तरह से समझने में मदद करता है, “शुरूआती मां-बच्चे की एकता का सच दूध छुड़ाने के वक्त खत्म हो जाता है. दूध छुड़ाने के इस पल में बच्चा अपनी ‘खुद की एकता की समझ और अहसास’ को खो देता है.” ब्रूस फिंक, जो एक और मनोविश्लेषक हैं, वे लाकां की परिकल्पना को प्यार के हवाले से आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि वे लिखते हैं,
[…] दो को एक में मिलाने की कोशिश, समय की सुइयों को पीछे धकेलना है. यह कोशिश उस पल में लौटने की जो अलगाव और जुदाई से पहले था […]
यह किसी गुम हो चुकी चीज़ के नुकसान को पलटने की कोशिश है, ऐसे प्रयास में जुटना कि जैसे कोई चीज़ खोई ही नही है. मां और बच्चे के बीच की दरार को ठीक करने का प्रयास.
हालांकि मां और बच्चे के बीच की दरार को कभी भी पार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कोई एकता थी ही नहीं, यह एक कल्पना थी. यह निरंतरता की फंतासी, खोई हुई एकता को फिर से पा लेने की चाह, प्रेम को सताती है.
कोई हैरत नहीं कि ई प्यार के “हरदम काफी न” होने के अहसास से हैरान थी. यह उन कई चौंकाने वाले सवालों में से एक था जो शोध के दौरान बार-बार सामने आए. इतने ज़्यादा कि हैशटैग्स की मुरीद न होने के बावजूद, क्योंकि वे हकीकत को जुमले में समेट देने का हुनर रखते हैं, इस हैरानी को हैशटैग्स में ज़ाहिर करना शायद सही होगा, #यह_कैसे_हो_सकता_है_कि_ये_कभी_काफी_नहीं_होता?
ऐसी ज़रूरत का बढ़ते जाना और हरदम कसर रह जाना हमें ‘कमी’ के बारे में मनोविश्लेषण की गहरी अवधारणा को समझने की ओर ले जाता है.
पैदा होना खुद में, कोख से दुनिया में आना, किसी भी जानवर से कहीं ज़्यादा बेसहारा होना, दूसरों के साथ से समर्पण करने की ज़रूरत, यानी बचपन से हममें कमी के निशान थे. पैदा होने का गहरा सदमा और इसके बाद मां के साथ ख्याली एकता के टूटने ने, हमारे नन्हें मन को अपनी ख्वाहिशों को कहीं और ले जाने के लिए मजबूर किया.
मनोविश्लेषण में, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है. कमी उतनी त्रासद नहीं है, जितनी यह सुनने में लगती है. असल में यही कमी ही है जो ख्वाहिशों को मुमकिन बनाती है. न केवल सेक्सुअल चाहत बल्कि हर तरह की इच्छा – चाहे वह प्यार, खाना, पहनावा, नौकरी, रहने की जगह, हमारे वोट वगैरह से जुड़ी हो. साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो, सारी इंसानी ख्वाइशें इसी कमी से उपजी हैं. (इस कमी को लाकां ने फ्रेंच भाषा में शब्द दिया है- manqué-a-etre. अंग्रेज़ी में इसे दो तरह से अनुवाद किया गया है. पहला, “होने में कमी” यानी ऐसी कमी जो वजूद में हो, जो किसी चीज़ के मिलने से पूरी नहीं हो सकती. दूसरा अनुवाद है, “ऐसा बनना चाहना” यानी एक मूलभूत ऊर्जा जो हमें पूरा होने की ओर धकेलती है.)
दार्शनिक और मनोविश्लेषक ज़ाक लाकां की बदनाम वज़नी बातों को आसान बनाते हुए, फिंक लिखते हैं,
जहां कोई कमी नहीं है, वहां कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती.
चाहत की भूमिका ये है कि ये इस कमी को पूरा करे या उस कमी की किसी और तरीके से भरपाई करे. हर एक नई चाहत जो उभरती है वो उसी पुरानी कमी के अहसास से ही जुड़ी हुई है या उसी का नया रूप है.
हालांकि, हमारी त्रासदी या विडंबना ये है कि ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रहेंगी. कसर रह जाने से ही ख्वाइश असर में है. इसे लाकां कहते हैं, “अधूरी ख्वाइश की ख्वाइश”.
अधिक सटीक रूप से, किसी के पूरे जीवनकाल में चाहत लगातार पीछा करती है, उस मायावी कुछ के लिए जिसे लाकां ने ‘ऑब्जेक्ट पेटिट ए’ कहा है और उस व्यक्ति के लिए, ये ऑब्जेक्ट पेटिट ए – जो ‘वो खोई वस्तु’ के नाम से भी जाना जाता है – उस प्राथमिक मूल नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है. ये एक स्थान धारक है और इसमें नामित वस्तु बदलती रह सकती है. यह नामहीन है और काफी मायावी है.
ताउम्र, यह चीज़ दूसरी चीज़ों, हवालों और माहौल में फैलती है. चूंकि यह केवल रोमांटिक और सेक्सुअल हसरत भर नहीं है जो किसी कमी से उत्पन्न होती है, बल्कि सभी इच्छाएं, खोजें हमें न केवल एक खास किस्म के प्रेमी की ओर ले जाती हैं बल्कि एक खास ढंग के सेक्स, खास नौकरियों, पसंदीदा रंग, पसंदीदा पोशाक, खास किस्म की तालीम, राजनीतिक विचारधारा, संगठन, या राजनीतिक नेता की ओर भी ले जाती है.
वस्तु शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि लाकां के मनोविश्लेषण में ‘पेटिट ऑब्जेक्ट ए’ कोई वस्तु नहीं है बल्कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति आकर्षित होता है. वस्तु खुद में नहीं बल्कि उसका वह पहलू जो हमारे भीतर एक खास किस्म की प्रतिक्रिया को उकसाता है जिसमें अचेतन से उपजी ऊर्जा होती है. इसलिए लाकां कहते हैं कि हरदम, चाहत की चाह को जारी रखना होता है. “चाहत एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर बढ़ती है[…] चाह खुद में एक मुकाम है: यह सिर्फ और चाहत की तलाश करती है, किसी वस्तु की नहीं.”
हमारी फंतासियां या कल्पनाएं लगातार उस खोई हुई वस्तु की तलाश में उमड़ती-घुमड़ती रहती हैं. सबसे अप्रत्याशित जगहों में उस खोई हुई वस्तु की झलक हमें मिल सकती है. सेक्सुअल और रोमांटिक कशिश के हवाले में, यह किसी की आवाज़ का लहजा या बालों को झटकने का ढंग हो सकता है जो हमें उनकी ओर आकर्षित करता है. कोई हैरत नहीं कि हमें पहली नज़र का प्यार और चाहत, बहुत कम समझ में आती है.
शायद मैं गलत हूं पर प्रेमी की कमी को पूरा करने के लिए अवचेतन तड़प उठती है और अपने अहसासों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराती है (हालांकि अहसास – इसलिए क्योंकि हम उनसे होशो-हवास में गुज़रते हैं – इसके दायरे में नहीं आते हैं).
मनोविश्लेषण हमें बताता है कि हम किसी एक मंज़िल तक नहीं पहुंच रहे. खोई हुई चीज़ की तलाश कभी खत्म नहीं होती है. और इस कमी को पूरा करना मुमकिन भी नहीं है.
ई हमें यह देखने की इजाज़त देती हैं कि प्यार कितने असरदार ढंग से अवचेतन के खेल को देखने में मदद कर सकता है – निरंतरता की तड़प, बार-बार की हताशा, कि हम जो खोज रहे हैं उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही पूरी तरह से शक्तिशाली लेकिन उत्तेजना से भरा हुआ वह क्षणिक अहसास कि हमने वह हासिल कर लिया है जिसकी हमें तलाश थी.
ई* पूरे नाम का प्रयोग न करके, पहले अक्षर का प्रयोग किया गया है.
इस लेख का अनुवाद पारिजात नौडियाल ने किया है.
पूरी शृंखला यहां पढ़ें.