हम, लोगों को जेल में इसलिए भी डाल देते हैं ताकि हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचना न पड़े. जेल के भीतर क्या होता है इसके बारे में शायद ही हम बात करते हैं या जानते हैं. जो जानते हैं वो उन फ़िल्मी ताकतवर नायकों के ज़रिए जो मार-मार कर अपराधियों की धज्जियां उड़ा देते हैं.
जेल के भीतर चीज़ें अलग-अलग तरीकों से होती हैं. हिंसा, जेल के अनुभवों का एक हिस्सा है. इसे कस्टोडियल वॉयलेंस यानी कैद में हिंसा कहा जाता है. इसमें पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दी गई यातना, मारपीट और यहां तक कि कैद में मौत शामिल है.
हिरासत में हिंसा के शिकार अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों से होते हैं, जैसे दलित, आदिवासी और गरीब. इन समूहों को सामाजिक पूर्वाग्रहों और शक्ति असंतुलन के कारण असमान रूप से निशाना बनाया जाता है.
कैद में हिंसा सिर्फ मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह कानून के शासन को भी कमज़ोर बनाने का काम करती है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी कम करती है. यह एक तरह से न्याय और हत्या के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है.
दक्ष – कानून, न्याय प्रणाली सुधारों, और न्याय तक पहुंच पर केंद्रित एक विचारमंच और शोध संस्थान है. दक्ष ने, पत्रकार और फ़िल्म आलोचक दीपांजना पाल के साथ बात कर एक पॉडकास्ट तैयार किया है, जहां वे हिरासत में होने वाली हिंसा और फ़िल्मों ‘पर’ एवं फ़िल्मों ‘का’ उसपर प्रभाव, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करे रहे हैं. दीपांजना का मानना है कि जेल के भीतर होने वाली हिंसा सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था की वजह से नहीं है जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं बल्कि यह हमारे भीतर गहरी धंसी सज़ा की चाहत का प्रतिबिंब भी है जिसे हमारे लोकप्रिय सिनेमा द्वारा प्रोत्साहित और व्यक्त किया जाता है. वास्तव में, जितना हम जानते-समझते हैं उससे कहीं अधिक लोकप्रिय सिनेमा का योगदान पुलिस हिंसा को सामान्य बनाने में हो सकता है.
हमारी फ़िल्मों में बार-बार यह देखने को मिलता है कि कैसे पुलिस बिना कोर्ट या किसी कानूनी कार्यवाही के अपना काम कर रही है और इसके लिए उनकी सराहना भी होती है. फ़िल्मों में ऐसे चित्रण को सही भी ठहराया जाता है, या एक तरह से हीरो की तरह दिखाया जाता है.
साहसिक पुलिसवाले के किरदार (जो अक्सर पुरुष होते हैं) कई भारतीय फ़िल्मों के केंद्र में होते हैं. ये किरदार जिन्हें आमतौर पर किसी लोकप्रिय कलाकार द्वारा निभाया जाता है और जो अक्सर पुलिस में अधिकारी होते हैं. ये बुराई से लड़ने के लिए नियमों को तोड़ते या मरोड़ते हैं. पुलिसकर्मियों को शारीरिक बल और यातना का इस्तेमाल करते हुए दिखाना, चाहे वो अपराध कबूल करवाने के लिए हो या अपराधियों को सज़ा देने के लिए, अक्सर नाटकीय तरीके से होता है, जो इस व्यवहार को बढ़ावा देता है.
हिरासत में यातना को हम सामान्य मान लेते हैं क्योंकि फिल्मों में जो पुलिसकर्मी यातना या बिना कानूनी सज़ा के हत्या करते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती. इसके बजाय, उन्हें रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, जिससे यह धारणा बनती है कि अगर नतीजा अच्छा हो तो तरीका कोई भी हो सकता है. इन फ़िल्मों में पुलिसकर्मियों का कानून अपने हाथ में लेना और खुद ही इंसाफ करना भी रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है.
असल में तो इन फिल्मों को न्याय व्यवस्था में घटते विश्वास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
लंबे-लंबे समय तक चलने वाले कोर्ट केसों के निपटारे में देरी, न्याय के प्रति लोगों में निराशा को बढ़ाती है. कुछ फिल्मों की कहानी इसी निराशा पर आधारित होती है, जो यह बताती है कि जब कानूनी व्यवस्था प्रभावी नहीं है, तो असली न्याय केवल कानून से बाहर जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है. ऐसे चित्रण लोगों के न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास को कम कर सकते हैं, और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जहां हिंसा को अपराध का सही समाधान माना जाता है.
यह भी सच है कि हर भारतीय फ़िल्म कैद में हिंसा का महिमामंडन नहीं करती. ऐसी कुछ सराहनीय फिल्में, जैसे ‘विसारनई’, ‘जय भीम’, और ‘मुल्क’, में पुलिस की बर्बरता और सुधार की ज़रूरतों के विषय को उठाया गया है. ये फिल्में कानून के अमल को एक गहरी समझ के साथ पेश करती हैं और जवाबदेही और मानवाधिकारों की अहमियत पर ज़ोर देती हैं. हालांकि, ये वैकल्पिक कहानियां अक्सर उन व्यावसायिक रूप से सफल एक्शन फ़िल्मों के आगे दब जाती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर छाई रहती हैं.
दक्ष पॉडकास्ट (DAKSH Podcast) आम जनता को सार्वजनिक संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने की कोशिश करता है. पॉडकास्ट के अब तक के तीन सीज़न में कई मुद्दों पर बातचीत सुनने को मिलती है. जैसे भारत में पुलिसिंग, संविधान सभा में महिलाएं, न्यायपालिका में एआई आदि. यह सीरिज़ विशेष रूप से मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में न्याय व्यवस्था की छवि पर असर का पता लगाने में रुचि रखती है. एक एपिसोड में निर्देशक चैतन्य तम्हाणे के साथ फ़िल्मों में कोर्टरूम के चित्रण पर चर्चा की गई है, और हाल ही में फ़िल्म आलोचक दीपांजना पाल के साथ फ़िल्मों में पुलिस हिंसा पर बात की गई है.
दक्ष पॉडकास्ट से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलीं, यह भी कि तमिल फ़िल्म निर्देशक हरि ने अपनी फ़िल्म सिंगम के लिए माफ़ी मांगी और उसके बाद ‘पांच ऐसी फ़िल्में बनाईं जो पुलिस के काम की सराहना’ करती हैं. यह पॉडकास्ट अंग्रेज़ी में है और इसे सुनने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.
इस बातचीत से कुछ महत्त्वपूर्ण विचार हम आपसे यहां साझा कर रहे हैं.

“60 से 80 तक के हिंदी सिनेमा में पुलिस का किरदार निभाने वाले हीरो के रूप में शायद ही दिखाई देते हैं. ऐसे किरदार अक्सर उलझनों में फंसे रहने वाले, अच्छे और कभी-कभी मज़ाकिया लोग होते थे. 80 के दशक से पुलिसवाले नायक की तरह दिखाए जाने लगे, लेकिन वे एक ऐसी दुनिया में होते हैं जो पूरी तरह से अराजक, अव्यवस्थित और टूट रही है."

“इस फ़िल्म की नायक रेखा हैं जो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस में भर्ती होती हैं. उनके पति एक पुलिस अफसर थे जिनकी रहस्यमय तरीके से एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है. 80 के दशक में, हिंदी फ़िल्मों में पुलिसवाले हालात से बंधे हुए नहीं होते थे. उनकी वर्दी और पुलिस की नौकरी उन्हें समाज को सुधारने की ताकत देती थी. आज ये काफी अलग है. आज के चित्रण में यह समाज को बदलने से ज़्यादा, कहानी कहने के तरीके से जुड़ा होता है."

"समाज में एक बड़ी आबादी जिस तरह की बेबसी और किसी भी तरह की ताकत के न होने के अहसास को महसूस करती है, इस फ़िल्म में पुलिसवालों को ठीक वैसा ही महसूस करते दिखाया गया है.”

"एक ऐसे पुलिसवाले का विचार जो बाकियों से अलग है, जो कानून का गलत इस्तेमाल करता है और फिर बाद में उसे सही करता है, यह एक ऐसी कहानी है जिसका सीधा संबंध राजनीति के भीतर देखा जा सकता है. निर्देशक रोहित शेट्टी का कहना है कि डर ज़रूरी है. यहां तक कि उनकी फंतासियों से भरी फ़िल्मों में भी डर केंद्र में होता है जिसपर फ़िल्म टिकी होती है.”

फ़िल्म समीक्षक दीपांजना पाल का कहना है कि “इसमें कैद के भीतर हिंसा को इस तरह दर्शाया गया है जैसे वो एक सच्चाई है.

“एक महिला पुलिस अधिकारी को गंभीर दिखने के लिए और ज़्यादा भयानक और हिंसात्मक चीज़ें करनी पड़ती हैं - जो ताकत की मर्दाना अवधारणा की पुष्टि करता है.”

पुलिस, चार बेकसूर मज़दूरों को चोरी का जुर्म कबूलने के लिए मजबूर करती है जो चोरी उन्होंने की ही नहीं है. विसारनई का मतलब है इंट्रोगेशन. "असल में तो हिरासत में हुई हिंसा को समझने के लिए पीड़ितों या गवाहों से बात करनी चाहिए ताकि सही समझ मिल सके. लेकिन इसके बजाय पुलिस रिकॉर्ड देखा जाता है क्योंकि वो आसानी से मिल जाते हैं. यहीं हमारी समझ गलत दिशा की ओर जाती है. कहानियों को पीड़ितों से बात करनी चाहिए ताकि उनकी आवाज़ को प्राथमिकता दी जा सके."
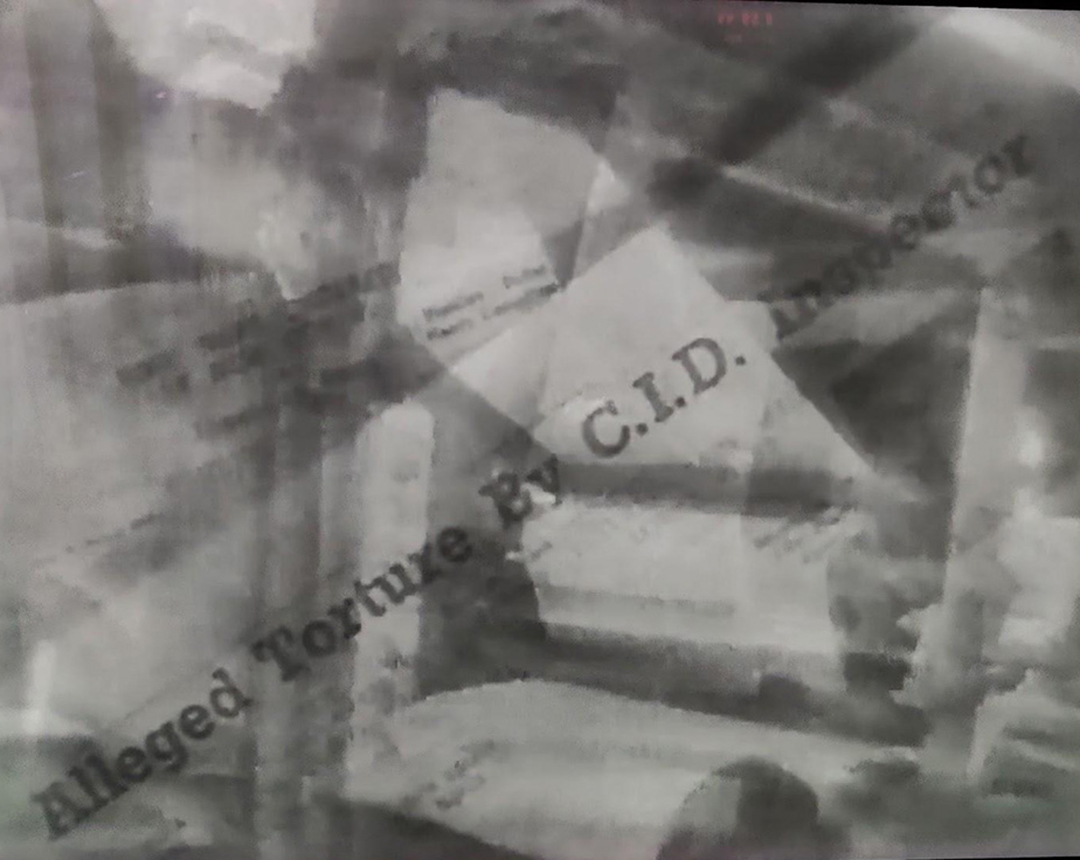
इस फ़िल्म में हिरासत में होनी वाली मौत का ज़िक्र दिखाई देता है. इससे पता चलता है कि बहुत पहले से ही इस तरह की बातचीत फ़िल्मों में हो रही थी. "आज के समय में कैद में होने वाली हिंसा बहुत बढ़ गई है. 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमानतः हर दिन हिरासत में पांच मौतें होती हैं, फिर भी इसके बारे में शायद ही कोई बात होती है. उदाहरण के लिए - तमिलनाडू के तूतीकोरन में 2020 में पी. जयराज और बेन्निक्स, पिता और पुत्र की हिरासत में मौत का मामला सार्वजनिक मंचों पर बहस का मुद्दा बना था लेकिन उसके बाद इस बारे में आगे कोई बात नहीं हुई."
इस लेख का अनुवाद सुमन परमार ने किया है.
द थर्ड आई की पाठ्य सामग्री तैयार करने वाले लोगों के समूह में शिक्षाविद, डॉक्यूमेंटरी फ़िल्मकार, कहानीकार जैसे पेशेवर लोग हैं. इन्हें कहानियां लिखने, मौखिक इतिहास जमा करने और ग्रामीण तथा कमज़ोर तबकों के लिए संदर्भगत सीखने−सिखाने के तरीकों को विकसित करने का व्यापक अनुभव है.




