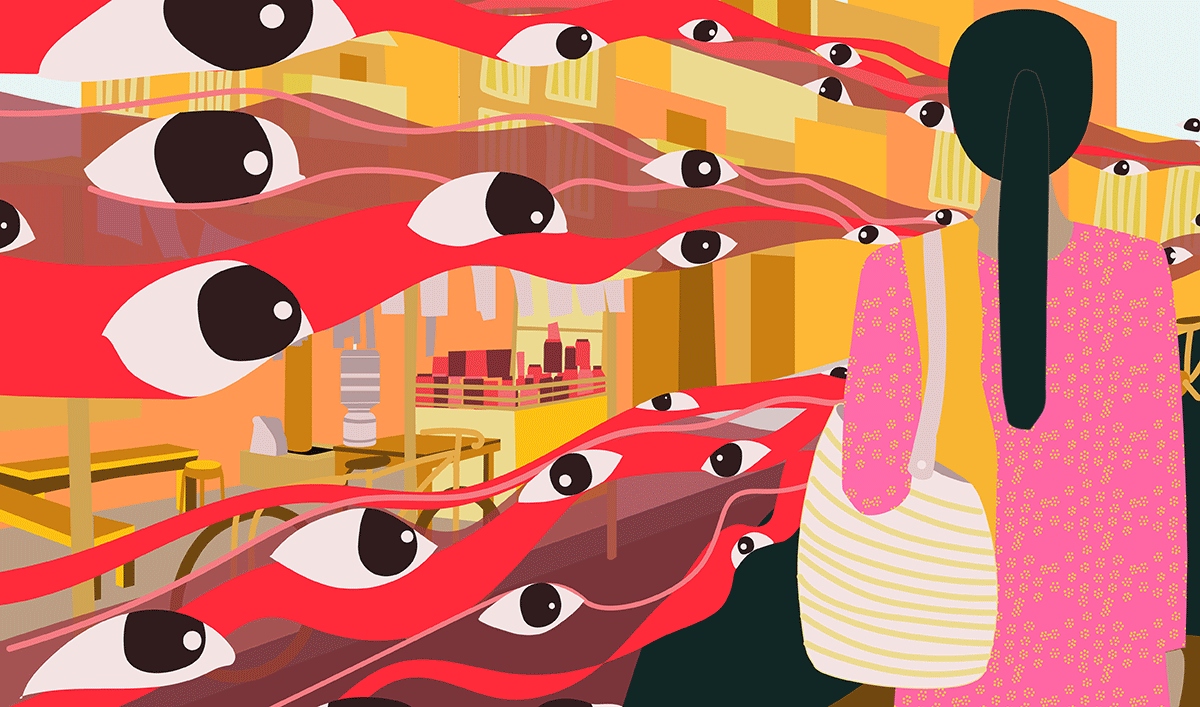पिछले एक साल में द थर्ड आई टीम ने उत्तर-प्रदेश के बांदा, ललितपुर और लखनऊ से जुड़ी 12 केसवर्करों के साथ मिलकर लेखन, थियेटर एवं कला आधारित शिक्षाशास्त्र (पेडागॉजी) पर काम किया. इस गहन प्रक्रिया से कुछ शब्द निकले और उनपर चर्चा करते-करते हिंसा की शब्दावली ने जन्म लिया. यह शब्दावली केसवर्करों द्वारा तैयार की गई है और यह उनके काम, अनुभव और ज़िंदगी के प्रति उनकी समझ और ज्ञान को समेटे हुए है.
बात उस दौर की है जब हमारी उम्र 16 साल की थी और अपनी मां और छोटी बहन का पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे थे. ऐसा करने पर हमें अपने परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की तरफ से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उस वक्त हम हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड (HLL) में सुपरवाइज़र के पद पर काम कर रहे थे. हम, रोज़ घर से निकलकर काम के लिए जाते. पर, असल में उस समय हमारे पास न तो हिम्मत थी और न ही आत्मविश्वास!
सुपरवाइज़र के बतौर हमारी ज़िम्मेदारी थी – घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के बारे में लोगों से जानकारी लेना. हर दिन हम अलग–अलग मोहल्ले में घर-घर जाते और जानकारी लेने के लिए लोगों से बात करते. यही वो वक्त था जब पहली बार हमें पहचान आधारित भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था.
पर वहीं, हमारे मोहल्ले वालों को लगता था – ये ऐसा कौन सा काम करती है जिसमें हर दिन इसे गली-गली घूमना पड़ता है?
सुपरवाइज़र की नौकरी में हमें 15,000 से 20,000 रूपए मिलते थे. इन पैसों को हम छोटी बहन की पढ़ाई, मां की दवाई और घर में राशन लाने, गैस भरवाने जैसी मोटी-मोटी ज़रूरतों पर खर्च करते थे. कहीं रिश्तेदारी में शादी पड़ती तो मां की तरफ से बड़ा तोहफा देना पड़ता था. उसका इंतज़ाम भी हम ही करते थे. हमारे भाई इसमें कोई मदद नहीं करते. उल्टे वे मां से कहते, “तुम्हारी बिटिया कमाती है उससे ले लो, मैं क्यों दूं.”
रोज़ घर से बाहर निकलते थे तो हमारे भी अपने खर्चे होते थे. तो, घर के सारे खर्चों के बाद जो कुछ थोड़े-बहुत पैसे बचते उन्हें हम खुद के लिए ढंग का कपड़ा और मोबाइल रीचार्ज करने में खर्च करते.
हमारे रहन-सहन को देख कर मोहल्ले वाले हैरान रहते और हमारी मां को हर दिन ताना देते कि अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो अपनी बेटी से काम करवा रही हैं. वे मां से कहते,
“बेटी की कमाई हराम है, तुम अपने अच्छे खान-पान के लिए अपनी लड़की को बाहर भेजती हो, वो गली-गली छछुंदर की तरह घूमती रहती है.”
उधर मेरे भाई से भी मोहल्ले के नुक्कड़ पर या चाय की गुमटी पर खड़े लड़के कहते कि तुम्हारी बहन तो बाहर जाती है. न जाने किस-किस से मिलती है, क्या करती है. उनमें से एक ने कहा, “सुना है, तुम्हारी बहन होटलों में जाती है. लगता है वो कोई धंधा करती है…” ये सब सुनकर जब मेरा भाई घर लौटता तो गुस्से से लाल रहता. उस वक्त उसकी आखें सिर्फ़ हमें तलाश रही होतीं कि रुकसाना (बदला हुआ नाम) मिल जाए तो आज उसे जान से मार डालूंगा.
रोज़-रोज़ के ये ताने-बातें सुनकर हमारा मन अक्सर दर्द में डूबा रहता. पर, दर्द में डूबे मन के साथ हम अगली सुबह फिर घर से बाहर निकलते और गली के नुक्कड़ पर खड़े लड़कों के माखौल का सामना करते नौकरी पर जाते. कभी, लड़कों की भीड़ में से कोई एक लड़का तेज़ आवाज़ में बोलता – देखो जा रही है होटलों में धंधा करने वाली.
धीर-धीरे इन तानों का हमारे ऊपर असर भी होने लगा. इनकी वजह से हमारा दिल भी अपने काम से बिल्कुल हटता जा रहा था. व्यक्तिगत रूप से हम हर वक्त टूटा हुआ महसूस करते. इसी बीच यह भी हुआ कि जिससे हम प्यार करते थे उसने धोखा दे दिया. हमें छोड़कर उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली. इस घटना ने हमें बहुत ज़्यादा तोड़ दिया. हम बहुत हताश और निराश थे. सिर्फ़, परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में नौकरी कर रहे थे क्योंकि यह भी फ़िक्र हमेशा बनी रहती कि मां की दवा और छोटी बहन की पढ़ाई कहीं बंद न हो जाए.
आज हम जहां हैं, इस सफ़र को तय करने में न जाने कितनी बार अनचाहे समझौते करते आए हैं. कभी गरीबी और मुफलिसी के नाम पर, कभी आगे नया रास्ता खोजने के नाम पर, तो कभी रिश्तों के नाम पर. समझौता, ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर हमारे इर्द- गिर्द घूमता ही रहा है.
पर, कभी-कभी समझौता मील के पत्थर का काम भी करता है. वो हमें एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर ले जाने का काम करता है. जहां कभी किसी मोड़ पर उलझन और टूटन से सामना होता है तो कहीं आगे बढ़ने के लिए नई रौशनी भी दिखाई देती है. पर, जिस समय भी समझौता करने की घड़ी आती है, तो मानो सीने पर बहुत बड़ा सा सिल रखकर ही ये समझौते किए जाते हैं. वहीं, ये भी सच है कि कुछ समझौते हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव भी लेकर आए हैं.
एक केसवर्कर की हैसियत से हमने इस बात को महिला हिंसा से जूझ रही महिलाओं की ज़िंदगियों में भी देखा है कि वे कितना मजबूर होकर समझौते करती हैं. मजबूरी की शक्ल में कभी उनके बच्चे होते हैं, कभी बीमारी, तो कभी सिर ढकने के लिए छत. ऐसे में उन्हें सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी वे तमाम मजबूरियां सामने दिखती है जो चीख–चीख कर कहती हैं कि समझौता ही मुझे बचा सकता है, समझौता ही मेरी बीमारी का इलाज हो सकता है, मेरे बच्चों का भविष्य हो सकता है!