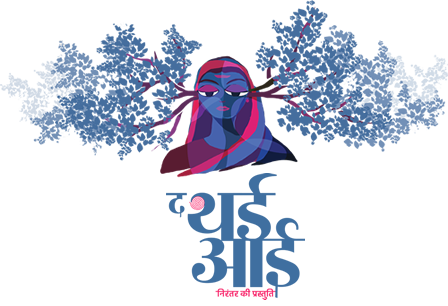एक विज्ञान शिक्षक के रूप में, जब आपने भारत में वर्षों के टीकाकरण अभियान के बाद भी कोविड के टीके को लेकर इतनी व्यापक हिचकिचाहट देखी तो आपने क्या महसूस किया?
मैं वैज्ञानिक चेतना और टीके को लेकर हिचकिचाहट, इन दोनों मुद्दों को आपस में उलझाना नहीं चाहूंगा. लेकिन मुझे लगता है कि वैज्ञानिक शिक्षा ने हमें बहुत बुरी तरह से निराश किया है.
सबसे पहले, टीके को लेकर लोगों की झिझक के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि लोगों ने तर्कसंगत विकल्प अपनाया. पहली लहर में बहुत कम मौतें हुई थीं. इसलिए लोगों- ख़ासकर वे जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है – को टीके की ज़रूरत महसूस नहीं हुई. लेकिन दूसरी लहर आई और झिझक काफ़ी तेज़ी से ग़ायब हो गई.
इसलिए मेरे ख़्याल में ये सोचना कि “क्या मुझे इसकी ज़रूरत है?”, यह एक बहुत ही तर्कसंगत हिचक है. और जब एकबारगी उन्होंने देखा कि दूसरी लहर लोगों को मार रही है, तो वे निश्चित रूप से टीका लेने के लिए कतारों में खड़े हो गए.
लेकिन, कोविड महामारी में जिस तरह से लोगों की जानें गईं उसका आकलन करने में हम नाकामयाब रहे, उसे देखते हुए मैं यह कहता हूं कि विज्ञान की शिक्षा ने हमें निराश किया है.
मैं केन्द्रीय विद्यालय स्कूल से हूं और केन्द्रीय विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकें बहुत अच्छी हैं. पर, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा से, वे मेडिकल, इंजीनियरिंग या आईएएस की परीक्षाओं की तैयारी या राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर आधारित पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित करने लगते हैं.
इसके बजाय, काश इन किताबों में ऐसी कार्यशालाएं होतीं जो स्टुडेंट्स को कहतीं कि चलो आज हम एक बस डिपो पर जाएं, या खेतों में काम कर रहे किसान से मिलें और पता करें कि उसकी पैदावार क्या है, या चलो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) जाकर, नर्स से बात करें, इस तरह हम इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नज़दीक से जान पाएंगे, जिससे लोगों को बहुत मदद मिलती है.
या फिर किसी आशा कार्यकर्ता के साथ समय बिताएं. आशा कार्यकर्ताओं के पास एक नोटपैड होता है जिसमें गांव के लोगों के नाम और उन्हें कौन सी बीमारियां हैं, किस परिवार को किस किस्म की स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी है, सब कुछ नोट किया जाता है. ऐसा क्यों है कि एक गांव में डायबिटीज़ के इतने रोगी हैं और दूसरे गांव में इसका कोई रोगी नहीं है?
इन्हीं वजहों से मुझे लगता है कि विज्ञान की शिक्षा ने जागरूकता से भरे इन विषयों की शिक्षा पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया.
क्या आप यह कह रहे हैं कि विज्ञान को हमारे जीवन के ठोस संदर्भों से बात करनी चाहिए?
मैं तो यह कह रहा हूं कि विज्ञान की शिक्षा का ताल्लुक सिर्फ़ विज्ञान के बड़े मसलों से नहीं है, और उसे विज्ञान के बड़े-बड़े मसलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए.
लेकिन, अगर आप केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक विभागों को देखें, तो वे- अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा से जुड़े हैं. ठीक है,
हमारे पास मिसाइल बनाने वाले पुरुष और महिलाएं हैं, विज्ञान के क्षेत्र में नामी-गिरामी लोग हैं. लेकिन हक़ीक़त में, दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में विज्ञान का मतलब सड़क, बिजली, पानी है.
आपको पता है अमरीका के एक विश्व प्रसिद्ध तकनीकी कॉलेज एमआईटी (MIT) में 1956 तक स्वच्छता इंजीनियरिंग विभाग हुआ करता था. 1956 में उन्होंने सोचा कि चूंकि उनके शहर मैसाचुसेट्स (अमरीका) में लंबे अरसे से अच्छे सीवर हैं, इसलिए हमें इस दिशा में अब किसी और शोध की ज़रूरत नहीं है.
लिहाज़ा मुझे लगता है कि किसी समाज विशेष की वास्तविक दिक्कतों को सामने खड़ा कर बात करना बेहद ज़रूरी है, “मेरा कुआं क्यों सूख जाता है?” या “मेरी बस देर से क्यों आती है?” मुझे लगता है कि विज्ञान की विषयवस्तु पूरे विश्व में एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसके कायदे या तरीके बेहद सांस्कृतिक (स्थानीय) हैं.
मुंबई विश्वविद्यालय में, हम एक केस स्टडी पर काम कर रहे हैं. हम गांवों में जाकर इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि 1000 हेक्टेयर वाले गांव में कितना चावल उगता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से उन्हें कितना मिलता है? कितना बिकता है? इस तरह, चावल की पैदावार से लेकर उसके बिकने और उपयोग में लाने का पूरा हिसाब निकाला जाता है. इस केस स्टडी ने बहुत सारे स्टुडेंट्स के मन में इस प्रक्रिया के प्रति रूचि पैदा की क्योंकि इससे वे एकदम से यह बात समझ जाते हैं कि उपज और ग़रीबी या निर्यात और स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है.
या हम उनसे पूछते हैं, "गांव में सबसे अच्छा चूल्हा कौन सा है?" यह सवाल सुन बहुत से स्टुडेंट्स हैरान होकर पूछते हैं, “क्या चूल्हा एक वैज्ञानिक वस्तु है?’ और मैं कहता हूं, “नहीं, लेकिन आप चूल्हे को अच्छा या बुरा कैसे कहते हैं?” इसका जवाब लड़कियां सबसे तेज़ी से देती हैं. वे कहती हैं, “एक अच्छे चूल्हे को तेज़ होना चाहिए” या “इसमें से कम धुआं निकलना चाहिए” या “इसे लकड़ी की कम खपत करनी चाहिए ...”
मुझे लगता है कि इस क़िस्म की पड़ताल, दस्तावेज़ीकरण, फील्डवर्क करना और उसमें कार्य-कारण स्थापित करना – वास्तव में ये विज्ञान के महत्त्वपूर्ण अंग हैं. विषयवस्तु भले ही परमाणु ऊर्जा हो या फिर “बस लेट क्यों है?”
क्या हमारे वैज्ञानिक संस्थानों को भी समाज के भीतर अपने स्थान के बारे में सोचने की ज़रूरत है?
निश्चित रूप से. उदाहरण के लिए, अगर आईआईटी का विश्लेषण किया जाए, तो वास्तव में कितने उच्च जाति के और कितने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं वहां? इसके साथ यह भी देखिए कि ये आईआईटी जैसे संस्थान जाति से जुड़ी हक़ीक़तों के बारे में क्या कर रहे हैं?
मतलब आप सामाजिक और भौतिक विज्ञान के बीच परस्पर संवाद की बात कर रहे हैं?
बिल्कुल. आपको मालूम है कि दोनों का यह विभाजन बहुत विरोधाभासी हैं… मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हैं, शायद डर है. इंजीनियर्स कहेंगे कि आपको प्रति वर्ष इतने किलो के भोजन की ज़रूरत है, या अगर मैं आपके सामने आपके बच्चे का वज़न करता हूं और वह बच्चा केवल छह किलो, या दस किलो का है और उसकी उम्र 10 साल की है, तो यह एक समस्या है. लेकिन क्या बच्चों में कुपोषण की समस्या को समझने का यही एकमात्र तरीका है?
बाहर के अधिकांश देशों में ऐसा कोई विभाजन नहीं है. मैं मानता हूं कि सामाजिक वैज्ञानिकों को हम इंजीनियरों की ओर देखना शुरू कर देना चाहिए और हमें भी सामाजिक वैज्ञानिकों की ओर अधिक रुचि और आलोचनात्मकता के साथ देखना चाहिए.
मैला ढोने को प्रतिबंधित करने वाला क़ानून बहुत पहले आया था और इसके साथ ही उन 42 उपकरणों की एक सूची आई थी, जो हर नगरपालिका के पास होनी चाहिए; एक मास्क, एक जेटिंग मशीन, पंप इत्यादि. हालत यह है कि आईआईटी के कैंपस में भी ये उपकरण उपलब्ध नहीं हैं.
क्या कोई ऐसी प्रयोगशाला है भी जहां ‘टेस्ट मास्क’ हो? हमारे लोग मैला टंकियों में जा रहे हैं और ज़हरीली गैसों के कारण मर रहे हैं. ‘टेस्ट मास्क’ एक किस्म का निवेश है. ये कितना असरदार है उसको समझने के लिए आपको एक चेहरे के आकार जैसी संरचना और विभिन्न वातावरणों के संपर्क में आने वाले नकली फेफड़े की ज़रूरत होती है. और इस मास्क को हर राज्य में एक मानक उपकरण के तौर पर उपलब्ध होना चाहिए.
लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने आईआईटी जैसी संस्थानों से भी करने के लिए कभी नहीं कहा, है ना? हमने कभी यह नहीं पूछा कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को कौन-सी दिक्कतें परेशान करती हैं. या महिलाओं को क्या चाहिए?
तो, आपके अनुसार भारतीय संदर्भ में विज्ञान के लिए आगे का रास्ता क्या है?
जिसे हम स्थानीय विज्ञान कहते हैं उस पर मैंने आईआईटी, बॉम्बे में एक टेडएक्स (TED EX) भाषण दिया था. आप स्थानीय इमारतों को ही देखें, यह लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाती हैं. इसी तरह, स्थानीय विज्ञान, वास्तविक समाधानों को उपलब्ध कराने से संबंधित है.
मेरे ख़्याल में विज्ञान महज़ हक़ीक़तों का अध्ययन करने का दावा करता है. अधिकांश हक़ीक़तें सामाजिक रूप से तय होती हैं और इसलिए, हमें इस किस्म की हक़ीक़त को भी विज्ञान के एक हिस्से के रूप में मानने की ज़रूरत है. स्थानीय विज्ञान असल में इस समय के ठोस सवालों को देखता है और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से हल करने का प्रयास करता है. अब वास्तविक सवाल यह है कि – कुआं क्यों सूख गया? कुआं बनाने के लिए परतों को निकालने की प्रणाली क्या है?
तो यह वाकई वो विज्ञान है, जो वास्तविक जीवन के प्रश्नों के समाधान के बारे में चिंतन करता है. यहां मैं स्थानीय शब्द का प्रयोग इस अर्थ में कर रहा हूं कि यह सवालों को हल करने वाला विज्ञान होना चाहिए.
एक दिलचस्प उदाहरण यह है कि एक स्टुडेंट के घुटने में चोट लगी थी, और वह दर्द से कराह रहा था. उसने एमआरआई करवाया और डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी. लेकिन क्या उसने डॉक्टर की सलाह मान ली? नहीं. ऑपरेशन करवाना है या नहीं इसके लिए वह अपने एक चाचा की सलाह पर भरोसा करता है.
इसलिए मुझे लगता है कि विज्ञान को सही तरीके से बरतने के लिए एक तीसरे पक्ष -सांस्कृतिक पक्ष की ज़रूरत है, अन्यथा यह स्वीकार्य नहीं होगा.
आजकल इलाज की विभिन्न पद्धतियों की बात की जा रही है, जो स्थानीय स्वास्थ्य के तरीकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने की बात करती हैं. क्या विज्ञान (विशुद्ध विज्ञान) इसके लिए राज़ी है?
क्या काढ़ा (जिसे मैं पीता हूं) काम करता है? या फ़िर तुलसी (जिसके पत्ते मैं खाता हूं) जकड़न को रोकती है? एक ‘वैज्ञानिक’ दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये एक अनावश्यक बहस है. आपको मालूम है कि अगर यह काम करता है, तो काम करता है.
अगर, हम एक कदम पीछे मुड़कर देखें तो विज्ञान के दो हिस्से हैं. पहला, क्या सच में कुछ काम करता है, और दूसरा कि क्या हम इसका कारण जानते हैं कि यह क्यों काम करता है. यह काम करता है या नहीं, से इस मुक़ाम पर पहुंचना कि क्या हम इसे समझा सकते हैं या नहीं, यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसे समझने में पश्चिमी विज्ञान को भी काफी समय लगा.
मसलन, 1800 के दशक में, यूरोप के एक सर्जन ने ग़ौर किया कि हाथों को धोने से वाकई मृत्यु दर को कम करने में मदद मिली, लेकिन उनके पास इस बात को साबित करने की कोई व्याख्या नहीं थी. सीनियर सर्जनों ने इस खोज की उपेक्षा कर कहा कि यह सच नहीं है. लेकिन फिर, लगभग 30-40 सालों बाद, उस बैक्टीरिया की खोज हुई और यह पाया गया कि यह वास्तव में सच है.
इसलिए, वैज्ञानिकों को भी यह स्वीकार करना होगा कि ऐसी कई चीज़ें हैं जिसे वे नहीं जानते हैं और यह अभी भी सच है. ऐसी बहुत सी बातें हैं, जो हम नहीं जानते. वैज्ञानिक, अनुभव और प्रयोगों के आधार पर काम करते हैं और कभी-कभी हम कहते हैं कि ठीक है, चलिए इसे अभी यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, और शायद बाद में हम इसके पीछे के 'क्यों' का पता लगा सकें. इस 'क्यों' या इसकी व्याख्या बेहद सांस्कृतिक है.
हम शरीर को कैसे देखते हैं यह भिन्न तरह के लोगों और संस्कृतियों के लिए काफ़ी अलग होता है. मसलन, जापान में, जब वे ‘मैं’ की ओर इशारा करते हैं, तो वे हमेशा नाक की ओर इशारा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी सांस ही “मैं” है. जबकि भारतीय अपने दिल की ओर इशारा करते हैं जब वे ‘मैं’ कहते हैं…
तो, हमें इन एक दूसरे से जुदा विचारों में से जो काम कर रहा है उसे स्वीकार कर इन भिन्न नज़रियों का दस्तावेज़ीकरण कर लेना चाहिए.
क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमारे विज्ञान और विशेष रूप से तकनीक ने प्रगति की है, विज्ञान की हमारी शिक्षा उस तरह की तकनीक की ओर अधिक झुक रही है जो वास्तव में समाज की ओर गंभीर रूप से देखने वाले विकास के मॉडल के बजाय बड़े व्यवसाय, कॉरपोरेट मुनाफे से जुड़े हितों को साध रही है?
हां, मुझे लगता है कि लोगों के वास्तविक सवाल अब विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं रहे. इन सब बातों को कहना अब बहुत ही अप्रचलित या दकियानूसी माना जाने लगा है. ऐसा कहने पर आपको गांधीवादी बता दिया जाएगा (जो मैं शायद नहीं हूं). मतलब यही है कि मूल ज़रूरतों की बातें करना प्रचलन से बाहर होता जा रहा है.
आज विज्ञान हमें कुछ और ही दे रहा है. मसलन हमारे जीने के सालों को ही ले लें. विज्ञान ने हमें आश्वस्त किया है कि वह हमें लंबे समय तक जीने में मदद करने में अपने वादे को पूरा कर रहा है. लेकिन जीवन के खाते में जुड़ने वाले ये पांच साल गुणवत्ता के आधार पर कैसे होंगे, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है.
उदाहरण के लिए, कोंकण जैसे सुंदर इलाकों से लोग मुम्बई की झुग्गी-झोपड़ियों में आकर रह रहे हैं क्योंकि वे निश्चितता चाहते हैं. ग्रामीण महाराष्ट्र में जीवन बहुत कठिन है. अगर, शहर में मैं एक चपरासी हूं या सुरक्षाकर्मी हूं, तो वो गांव में रहने की अपेक्षा अधिक निश्चितता देता है.
इसलिए मुझे लगता है कि विज्ञान वास्तव में कुछ ‘निश्चितता’ प्रदान कर रहा है. और इस बात को हमने स्वीकार भी कर लिया है. यह निश्चितता कई वैज्ञानिक चीज़ों से आ रही है, जिन्हें हम नहीं समझते और जो बड़े-बड़े विज्ञान द्वारा प्रदान की जाती हैं.
चीजें ‘कैसे’ और ‘क्यों’ काम करती हैं, इससे जुड़े सवालों को बेअसर करके बड़ी तकनीक ने हम सभी को विज्ञान के उपभोक्ता के रूप में तब्दील कर दिया है.
हम इसे स्वीकार कर, इसके फ़ायदों का आनंद लेते हैं. लेकिन आप देखिए, यदि आप जानते हैं कि प्रॉफिट बहुत ग़ैर-बराबर तरीके से विभाजित किया जाता है, तो यह हमें परेशान क्यों नहीं करता? उदाहरण के लिए, अगर आप 1000 डॉलर (74 हज़ार रूपए) में एक एप्पल आईफोन ख़रीदते हैं, तो फ़ोन के वास्तविक निर्माताओं (फैक्ट्री मज़दूर) को कितना मिलता है?
मैं इसे ‘बुद्धू-बनाने’ का संकट कहता हूं. बहुत सारे लोग बस अपने स्मार्टफोन में ही जीते हैं और एक बने-बनाए, तयशुदा निश्चितता के बुलबुले में रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ़ समाज के बाक़ी हिस्से को, जिसकी पहुंच स्मार्टफोन तक नहीं है, वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है.
‘बुद्धू-बनाने’ के इस संकट के बारे में हमें थोड़ा और बताइए?
मैं पक्षी प्रेमी हूं, और अगर आप जंगल को देखें तो, जंगल के तरीकों को नज़रअंदाज़ करने का मतलब है कि कोई भी जानवर अगले ही पल अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता है. क्या आप ऐसे किसी हिरण की कल्पना कर सकती हैं जो यह नहीं पता लगा सकता कि बाघ उसके कितने करीब पहुंच चुका है? अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वो बाघ का भोजन बन जाएगा! लेकिन हम इंसान अपने साथ ऐसी धूर्तता बरकरार रखते हैं जिसमें हमें अपने जीवन से जुड़े भौतिक तरीकों का भी अंदाज़ा है.
भले ही हम लंबे समय तक जी रहे हैं, लेकिन हम अभी भी सड़कों के किनारे पर शौच कर रहे हैं या अपने सीवर की सफाई, किसी दूसरे इंसान से उसकी जान को जोख़िम में डाल कर करवा रहे हैं! लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम लंबे समय तक जी रहे हैं न! और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है.
ये दो या तीन चीज़ें हैं, जो मेरे लिए सीख का काम करती हैं. मुझे लगता है कि यहां हमारी संस्कृति और स्थिरता की भूमिका वाकई बेहद महत्त्वपूर्ण है.
क्या आप यह कह रहे हैं कि विज्ञान हमें निश्चितता प्रदान कर सकता है? विज्ञान और हमारी चाहतों के बीच क्या संबंध है?
मुझे हर मौसम में आम चाहिए या मुझे 35,000 फीट की ऊंचाई पर स्ट्रॉबेरी का जूस चाहिए. मेरा मतलब उस निश्चितताओं से है जो हमारी इच्छाओं से निकल कर आती हैं, और विज्ञान का यह बड़ा रूप इसे पूरा भी कर रहा है. हमने जिन दवाइयों का अविष्कार किया है उसपर ग़ौर करें. वे हमें कुछ भी करने में सक्षम बनाती हैं. अब हमारा समाज जोखिम वाला नहीं, इच्छाओं वाला समाज बन गया है.
हमारे जन स्वास्थ्य संस्करण के माध्यम से, हमने यह महसूस किया कि विज्ञान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मदद नहीं कर रहा है, वो ग़रीबों की सेवा नहीं कर रहा है. बदले में, ग्रामीण समुदायों से विज्ञान की अपेक्षा भी कम होती है. क्या आपको यह सच लगता है?
मुझे लगता है कि यह काफी हद तक सच है. लेकिन इसका ग्रामीण होने से कोई लेना-देना नहीं है. आप पश्चिमी महाराष्ट्र को देखें- पुणे नासिक बेल्ट. तो वहां कुछ बहुत समझदार लोग रहते हैं. वे मूल रूप से शहरी बड़े बाज़ारों के लिए सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं. सतारा, सांगली सिंचाई वाले क्षेत्र हैं. और वास्तव में, आप देखेंगी कि वे अपने भविष्य को लेकर बेहद सावधान हैं और समाज में अपनी जगह और राज्य की भूमिका को समझते हैं. और वे राज्य या सरकार से बहुत सी चीज़ों की उम्मीद करते हैं, वे चाहते हैं कि चीज़ें काम करें, अस्पताल काम करें, ऑक्सीजन उपलब्ध हो आदि.
एक किसान के लिए मुश्किल है कि वह कैमिकल इंजिनियर, या एक सिंचाई इंजीनियर और एक अर्थशास्त्री बने. यहां वह विज्ञान से उम्मीद करता है, कि वो उसके रोज़मर्रा के काम की शैली को बेहतर बनाने के तरीके उसके लिए इजाद करे. ज़्यादातर लोग जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वे बुद्धू नहीं हैं. लेकिन उन्हें अभी भी यह समझने की ज़रूरत है कि राज्य कैसे काम करता है.
इसलिए, आपके प्रश्न पर वापस लौटते हुए मुझे लगता है कि यह इस बात से भी जुड़ा है कि हम विज्ञान को कैसे देखते हैं.
इस लिहाज़ से, हमारा विज्ञान सच्चाई में – बाहर निकलने का रास्ता देने वाला विज्ञान है. विश्व इकॉनमी में आईआईटी एक लाइफबोट या बाहर निकलने वाले रास्ते की तरह है. हम जानते हैं कि 1 फीसदी इसपर चढ़ जाएंगे, 1 फीसदी इसका अध्ययन करेंगे और 1 फीसदी ही बाहर निकल पाएंगे और बाहर निकलने का यह रास्ता ही विज्ञान है.
इसलिए, हमारा विज्ञान वास्तव में एक पासपोर्ट विज्ञान है कि कैसे यहां से भाग निकलना है और उस स्थान को सुधारना नहीं है जहां मैं अभी हूं.
इस लेख का अनुवाद जितेन्द्र कुमार ने किया है.